बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उन प्रसिद्ध बाघों के लिए अत्यंत लोकप्रिय है जो अधिकतर पर्यटकों को अपने अद्वितीय दर्शन देकर तृप्त कर देते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्यजीव उद्यान का नाम सुनते ही मन मस्तिष्क में एक घने वन की कल्पना उभर कर आ जाती है जहां केवल वन्य प्राणियों का वास होता है, तथापि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान केवल एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बांधवगढ़, इस नाम को ध्यानपूर्वक पढ़ें। बांधव का अर्थ है बंधु व सखा तथा गढ़ का अर्थ है महल अथवा दुर्ग। क्या इस राष्ट्राय उद्यान में कोई गढ़ अथवा दुर्ग है? जी हाँ। इस वन के भीतर, एक विशाल चट्टान के ऊपर एक दुर्जेय गढ़ है जिसकी ऊँचाई ८११ मीटर है।
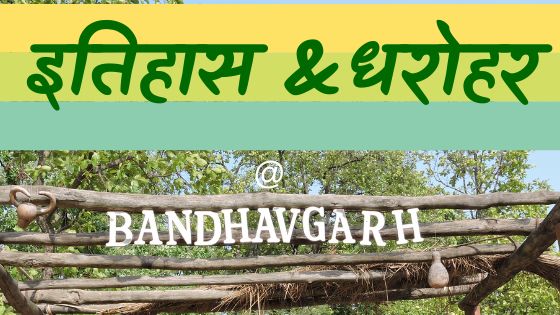
जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है, उसका शीर्ष सपाट मंच सदृश है जो इस पहाड़ी को एक आवास योग्य पठार बनाता है। आप इस पहाड़ी को वन के ताला एवं मागधी दोनों क्षेत्रों से देख सकते हैं। इस दुर्ग एवं इसकी धरोहर के दर्शन के लिए विशेष मार्ग पर जाना पड़ता है। मुझे भी यहाँ की धरोहरों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अनमोल ऐतिहासिक धरोहर

भारत की अधिकाँश किवदंतियों के समान इस स्थान का सम्बन्ध भी महाकाव्य रामायण से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यह दुर्ग भगवान राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण का था जिसके कारण इसका नाम बांधवगढ़ पड़ा। यहाँ से प्राप्त कुछ प्राचीन ब्राह्मी शिलालेखों के आधार पर पुरातत्वविद इसे ईसापूर्व युग का मानते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य दुर्ग की संरचना को १०वीं सदी का मानते हैं जो यह दर्शाता है कि यह दुर्ग ज्ञात ऐतिहासिक काल तक अनवरत बसा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि बघेल वंश के शासकों ने १७वीं सदी के आरम्भ तक इस गढ़ से शासन के कार्यभार का निर्वाह किया था, जिसके पश्चात उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ से १२० किलोमीटर दूर रीवा में स्थानांतरित कर दी थी। इस दुर्ग पर अब भी राज परिवार का स्वामित्व है।

सिद्धबाबा मंदिर
वन के भीतर श्रद्धा का प्रथम चिन्ह जो मैंने देखा, वह था एक छोटा सा सिद्धबाबा मंदिर, जिसके भीतर एक शिवलिंग एवं त्रिशूल था। यह स्थान बाघों के दर्शन के लिए भी लोकप्रिय है। वाहन द्वारा यहाँ के कुछ दूर जाते ही हम बांधवगढ़ पहाड़ी पर चढ़ने लगे थे। दूर से ही पहाड़ी पर मानव निर्मित संरचनाएं दृष्टिगोचर होने लगी थीं। मैंने अपने कैमरे को जूम करते हुए एक मंदिर देखा जो एक मध्ययुगीन संरचना प्रतीत होती है। तीव्र ढलुआ मार्ग गुफा जैसी संरचनाओं के सामने से जाता है। विशाल चट्टानों को काटकर ये स्तम्भ युक्त कक्ष निर्मित किये गए हैं जिन्हें देख ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ मानव एवं वन्य प्राणी दोनों आश्रय लेते हैं। वे इन संरचनाओं के विषय में क्या धारणा रखते हैं, यह मेरी कल्पना के परे है।
शेषशायी भगवान विष्णु की प्रतिमा

पहाड़ी के शीर्ष की ओर जाते समय, आधी पहाड़ी चढ़ते ही हमारी सफारी जीप जलकुंड के समक्ष रुक गयी। यह जलकुंड एक बावड़ी के समान है। इस जलकुंड के पृष्ठभाग में सुप्रसिद्ध शेषशायी की प्रतिमा है। अर्थात् शेषनाग के ऊपर योगनिद्रा में लीन भगवान विष्णु। ३५ फीट लम्बी इस प्रतिमा को एक ही शिला में उत्कीर्णित किया गया है। १०वीं सदी में निर्मित इस प्रतिमा का श्रेय कलाचुरी राजवंश के राजा युवराजदेव के मंत्री गोल्लक को दिया जाता है।

इस क्षेत्र में बहती सरिता को चरण गंगा कहते हैं, जिसका अभिप्राय है, भगवान विष्णु के चरणों के समीप से बहती गंगा। इस नदी का प्राचीन नाम वेत्रावली है। यह नदी आज भी वन एवं यहाँ बसे गाँवों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्त्रोत है।
शिव एवं ब्रह्मा
बांधवगढ़ वन में भगवान विष्णु अकेले विराजमान नहीं हैं। यहाँ उनका साथ देने के लिए ब्रह्माजी एवं शिवजी भी हैं। विष्णु के समीप एक सादा किन्तु बड़ा शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के समीप विष्णु की नरसिंह अवतार की प्रतिमा है। मुझे बताया गया कि एक कोने में ब्रह्मा की प्रतिमा है। कोने में कुछ शिल्पकारी थी किन्तु मैं उसमें ब्रह्मा की छवि नहीं देख पायी। जलकुंड के समीप ऊपर जाती सीढ़ियाँ हैं जिससे आप पहाड़ी के ऊपर चढ़कर चारों ओर के परिदृश्यों का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। ऊपर से देखने पर आपको जलकुंड के चारों ओर छोटी छोटी अर्धगोलाकार सुन्दर सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। चारों ओर के वृक्षों के जल पर पड़ते प्रतिबिम्ब अप्रतिम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये प्रतिबिम्ब पुनः आपको स्मरण करा देते हैं कि आप अब भी वन में ही हैं।
और पढ़ें – बाघ गुफाएं और उनके अद्भुत भित्तिचित्र व ठप्पा छपाई
मुझे ज्ञात हुआ कि पहाड़ी पर अधिक ऊपर जाने पर दुर्ग के विभिन्न भागों में विष्णु के अनेक अवतारों की प्रतिमाएं उत्कीर्णित हैं। विभिन्न सूत्रों के अनुसार दिवाली एवं जन्माष्टमी के अवसरों पर शेषशैय्या के समीप उत्सव आयोजित किये जाते हैं। ये दोनों दिवस विष्णु के दो अवतारों से सम्बंधित हैं, राम एवं कृष्ण। किन्तु वन विभाग के कड़े नियमों देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यहाँ भव्य स्तर पर उत्सव आयोजित किये जाते होंगे। मैंने मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग के वेबस्थल पर कबीर मेले के विषय में पढ़ा था जो दिसंबर मास में पहाड़ी के ऊपर मनाया जाता है। किन्तु वहां कोई मुझे यह जानकारी नहीं दे सका कि ये उत्सव अब भी मनाया जाता है अथवा नहीं।
बांधवगढ़ के भीतर के गाँव

मेरे बांधवगढ़ भ्रमण की कालावधि में एक दुपहरी हम रान्छा गाँव गए जो हमारे होटल किंग्स लॉज से अधिक दूर नहीं था। हमने पैदल भ्रमण करते हुए इस गाँव को समीप से देखा। पाठशाला का भवन किंचित जीर्ण था किन्तु वहां के घर सुन्दर थे। मुझे हमारे परिदर्शक के स्नेही, श्रीमती मुन्नी के घर के भीतर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उनका घर विशाल था। परिसर में कुआँ एवं खेत भी थे। मुन्नीजी अपने नातिन की देखभाल करते हुए अपने बड़े घर, कुआँ व खेतों की देखरेख भी कर रही थीं। उनके घर में अप्रतिम रूप से सजा गलियारा था। प्रत्येक कक्ष के प्रवेश द्वार को प्लास्टर अथवा गचकारी द्वारा अलंकृत किया गया था। द्वार के चौखट के ऊपरी भागों पर मिट्टी की उभरी हुई शिल्पकारी हैं। हमें शीघ्र ही यह ज्ञात हुआ कि इन रंग-बिरंगी प्रतिमाओं को घर के कर्ता पुरुष अर्थात् मुन्नी जी के पतिदेव ने उत्कीर्णित किया है।

हम घर के गलियारों में घूमते हुए उस पर किये गए कलाकारी को सराहते जा रहे थे। इस प्रकार के घर को समीप से देखना हमारे भूतकाल के अवशेषों को देखने के समान था। मिट्टी के चूल्हे, अब भी उपयोग में लाया जा रहा कुआं इत्यादि हमें हमारे पूर्वकाल का स्मरण करा रहे थे।
और पढ़ें – मुन्ना बाघ – मध्यप्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का प्रसिद्ध सितारा
रान्छा गाँव के इस घर पर की गयी कलाकारी को देख कर मुझे मध्यप्रदेश के सरगुजा जिले की प्रसिद्ध कलाकार सोनाबाई रजवार का भी स्मरण हो आया जिनकी अद्भुत कला का उदहारण मैंने रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में देखा था। यहाँ की कलाशैली भी उसी प्रकार की है जिसमें गचकारी द्वारा भित्तियों एवं द्वार के चौखटों पर उभरी हुई आकृतियाँ चित्रित की गयी हैं। यद्यपि दोनों कलाकृतियों के स्तरों में भिन्नता थी तथापि ये कलाकृतियाँ छत्तीसगढ़ समेत इस सम्पूर्ण क्षेत्र की उत्तम लोककला का स्पष्ट अनुमान प्रदान करती हैं। ये कलाकृतियाँ यह दर्शाती हैं कि कैसे इस क्षेत्र के आदिवासी अपने सादे घरों को अपनी कला के रूप में स्वयं का एक अस्तित्व प्रदान करते हैं। कैसे गाँव के स्त्री-पुरुष अपनी रचनात्मकता को उजागर करते हुए अपनी कलाक्षमता को गर्व से प्रदर्शित करते हैं, यह अनुसरणीय है।
बांधवगढ़ की बैगा जनजाति

मेरी तीव्र अभिलाषा रहती थी कि मैं मध्य भारत के कुछ आदिवासी जनजातियों से भेंट कर सकूं। मेरी यह अभिलाषा छोटी मात्रा में उस दिन पूर्ण हुई जब बैगा जनजाति के कुछ सदस्यों से मेरा साक्षात्कार हुआ। यद्यपि मैं उनके गाँवों के दर्शन नहीं कर सकी, तथापि हमारे आयोजक ‘पगडंडी सफारी’ ने एक नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया जिसमें बैगा जनजाति के सदस्यों ने कुछ पारंपरिक नृत्यों का प्रदर्शन किया था। उन्होंने विवाह समारोहों में गाये जाने वाले पारंपरिक गीतों पर लोकनृत्य किये। वे लयबद्ध गति से गोलाकार आकृति में घूमते हुए नृत्य कर रहे थे। कुछ क्षणों के पश्चात उनकी मुद्राएँ हमें भी समझ में आने लगीं। हममें से कुछ ने उनके साथ नृत्य करने की पहल की। उनकी मुद्राएँ भले ही समझ आ जाएँ किन्तु उन्हें प्रदर्शित करने की शक्ति हम कहाँ से लायेंगे? शीघ्र ही थक कर हमारे साथी पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। नृत्य के अंतिम भाग में नृत्य संघ के पुरुष सदस्यों ने आश्चर्यजनक करतब प्रदर्शित किये जिन्हें देख हमारी आँखें फटी की फटी रह गयीं।
बैगा जनजाति का भव्य रूप
दो दिवसों के पश्चात हमें बैगा जनजाति के सदस्यों को उन के भव्य परिधान एवं अलंकरण के साथ देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी भव्य केशसज्जा, वैभवशाली आभूषण तथा रंगबिरंगे वस्त्र व परिधान अद्भुत व दर्शनीय थे। स्त्रियों ने गले में जो चाँदी के हार धारण किये थे उन्हें सुतिया कहते हैं। मुझे वे हंसली समान प्रतीत हो रहे थे। वयस्क स्त्रियों व पुरुषों ने टखने में मिश्र धातु द्वारा निर्मित भारी कड़े पहने हुए थे। मुझे बताया गया कि बैगा आदिवासी ये कड़े तभी धारण करते हैं जब उन्हें अपने परिवार एवं समाज के अनुभवी व सयाना माना जाता है। अतः आप किसी भी बैगा युवक अथवा युवती को यह कड़ा धारण करते नहीं देखेंगे। यह एक प्रकार का संकेत है कि कड़ा धारक बैगा समाज का एक सम्माननीय व्यक्तित्व है। उनके परिधानों ने भी मेरा ध्यान आकर्षित किया। उनकी देह पर वस्त्रों की अनेक परते थीं। मध्य भारत के उष्ण तापमान में आदिवासी जीवन जीते हुए ऐसे वस्त्रों का परिधान अचरज कारक है। मैं सोच में पड़ गयी कि क्या ये उनके दैनिक वस्त्र हैं अथवा उन्होंने प्रदर्शन के लिए इन्हें धारण किया है?

मेरे सहयात्री पुनीत ने मेरी शंकाओं की पुष्टि की। बैगा जनजाति ने ऐसे भारी परिधानों को नृत्य प्रदर्शनों के कारण स्वीकार किया है। अन्यथा वे इस प्रकार के वस्त्र धारण नहीं करते हैं। सामान्य जनजीवन में ना स्त्रियाँ सर पर तुरे धारण करती हैं, ना ही पुरुष भारी अंगरखे धारण करते हैं। ना जाने केवल प्रदर्शन के लिए उन्होंने यह रूपांतरण क्यों किया तथा वे किससे प्रभावित हुए है? ऐसे अनुभवों से यह प्रश्न उठता है कि वास्तव में प्रामाणिक एवं मूल परंपरा क्या है? क्या हम परिकल्पित अवधारणाओं को इतना महत्त्व देते हैं कि मनुष्य अपनी परंपरा को त्याग कर काल्पनिक व्यक्तित्व को धारण कर ले?
और पढ़ें – मध्य प्रदेश के भील जनजाती का भगोरिया उत्सव
मैंने बैगा जनजाति के एक पुरुष को उसके मूल पारंपरिक परिवेश में देखा जब वह वन्य क्षेत्र के भीतर छोटे छोटे पौधे बीन रहा था। उसके सर पर बड़ी टोपी, कटि पर छोटी धोती, हाथ में कुल्हाडी थी तथा कंधे पर कपडे का बस्ता था।
बांधवगढ़ वन के विभिन्न तत्व
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के विभिन्न तत्वों को एक साथ देखकर मेरे मन मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर कर आ रहे थे। उद्यान का वन्य जीवन, आदिवासी जनसँख्या, गाँव, खेत, विभिन्न कला शैलियाँ, पहाड़ी दुर्ग, मंदिर, जलस्त्रोत एवं इसकी जैव-विविधता, इन सब को एक चौखट में देखने का बांधवगढ़ एक स्वर्णिम अवसर है। इन्हें देख मैं सोच में पड़ गयी कि कब व कैसे हमने प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्यता से जीवन निर्वाह करने की कला को विस्मृत कर दिया है? प्रकृति कब से हमारे लिए इतनी गौण हो गयी है? मनुष्य ने कब से यह धारणा बना ली है कि वही इस प्रकृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है तथा वह इसके अन्य तत्वों के साथ मनमाने ढंग से खिलवाड़ कर सकता है? वह भी केवल अपने क्षणभंगुर व्यक्तिगत संतुष्टि व अभिमान के लिए?
इस पर विचार एवं कृत्य अत्यावश्यक है।




















One of the most wonderful tourist places I have visted so far!
Me too Neena ji
Seems to be very beautiful and peaceful place. Nicely penned article
Thank you Radha Ji. Yes, Bandhavgarh is a beautiful mix of history, heritage and nature.