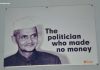मध्य एशिया में सदियों पूर्व पनपी बौद्ध संस्कृति के कुछ उत्कृष्ट अवशेष लद्दाख के हेमिस मठ की गोद में संरक्षित हैं। लद्दाख की हिमालयीन शुष्क पर्वतीय मरू भूमि की घाटियों में गर्व से खड़ा यह उत्तुंग मठ एक पावन धार्मिक आश्रम है जो नरोपा के आशीष से फलता फूलता है। नरोपा एक प्राचीन बौद्ध विद्वान थे जिन्होंने नालंदा महाविहार के कुलाधिपति के रूप में इस मठ के संचालन की अध्यक्षता की थी।
हेमिस मठ कहाँ है?
हेमिस मठ लेह नगर से लगभग ४५ किलोमीटर दूर स्थित है। इस मठ ने अपने ऊपर किये गए अनेक ऐसे आक्रमणों को सफलतापूर्वक निष्फल किया है जिन्होंने एक काल में मध्य एशिया को झकझोर कर रख दिया था। दूर से यह मठ दिखाई नहीं देता है। जब तक आप पर्वत की तलहटी तक नहीं पहुँच जाते तथा आतंरिक भागों में प्रवेश नहीं कर जाते, यह मठ पर्वतों की परतों में मानो ओझल रहता है। बाहरी विश्व के लिए यह मठ लगभग अदृश्य है।

यह मठ गांधार काल की कलाकृतियों से समृद्ध प्राचीन संस्कृति, बुद्धिमत्ता व विद्वत्ता का एक अज्ञात विश्व है। हेमिस मठ के परिसर में प्रवेश करते ही मठ की समृद्ध सांस्कृतिक संपत्ति की झलक मिलने लगती है। आप जैसे जैसे मठ की वैशिष्ट्यता की परतें खोलते जायेंगे, आपको यह अनुभव होगा कि प्रौद्योगिकी विकास द्वारा समूचे आधुनिक विश्व के स्वरूप में होते अनवरत परिवर्तन से यह मठ लगभग पूर्णतः उदासीन है। अनभिज्ञ है।
इसके पश्चात भी यह मठ स्थानिकों एवं बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय अनुयायियों पर छाये इसके प्रभावशाली प्रभाव की सीमा में ही पनपते नहीं रहना चाहता है। वस्तुतः, इसने सम्पूर्ण विश्व के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। यह अब पूरे संसार के तीर्थयात्रियों, शोधकर्ताओं तथा पर्यटकों को आमंत्रित करता है ताकि धार्मिक ग्रंथों व लोक साहित्यों के रूप में संरक्षित अपनी समृद्ध धरोहर तथा संस्कृति को वह सबके साथ बाँट सकें। नरोपा उत्सव उनके इस अनोखे प्रयास का प्रमुख उदहारण है।
दृक्पा थुक्से रिन्पोचे द्वारा लद्दाख में आत्मनिर्भर चिरस्थाई पर्यटन का आरम्भ
महानुभाव दृक्पा थुक्से रिन्पोचे मठ के प्रमुख संरक्षकों में से एक हैं। उन्होंने मठ में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण आयोजनों का आरम्भ किया है जो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर चिरस्थाई पर्यटन सुनिश्चित करेंगीं। वर्षों से संघर्षरत क्षेत्र में स्थित होने के पश्चात भी इन पर्वतों में छाई शान्ति को सदैव अखंडित रखने की ओर यह मठ निरंतर कार्यरत रहता है। साथ ही, यह मठ इस क्षेत्र के स्थानिकों के उत्थान के लिए भी सतत प्रयत्नशील रहता है। इन सब का स्थानीय युवाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

नरोपा उत्सव विभिन्न धर्मों एवं आस्थाओं का पालन करने वाले लोगों का एक अद्भुत एवं सफल संगम है जो इस उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर के गाँवों से आते हैं, वह चाहे लद्दाख का सुदूर गाँव हो या भूटान के पर्वतीय क्षेत्र हों अथवा भारत के मैदानी क्षेत्र। इस उत्सव में भाग लेते हुए, कुछ ही दिनों में हमने अनेक पर्यावरण प्रेमियों, धार्मिक विद्वानों, विभिन्न शैलियों के कलाकारों तथा ऐसे ही अनेक महारथियों से भेंट की। वे सभी के सभी इस विश्व में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए इच्छुक एवं तत्पर थे।
सिन्धु नदी
लेह से हेमिस मठ की ओर जाते हुए आपका साक्षात्कार भव्य सिन्धु नदी से होता है। सिन्धु नदी भारतीयों का मान भी है एवं परिचय भी। सिन्धु नदी के कलकल बहते जल को निहारना सम्मोहित सा कर देता है। पर्वतों के ऊपर, सिन्धु नदी के तट पर अनेक बौद्ध मठ स्थित हैं।
और पढ़ें: लेह से लद्दाख तक सड़क यात्रा – शीत ऋतु में लद्दाख
विलो अथवा धुनकी के झाड़, चिनार के वृक्ष, झूमती इठलाती नदी तथा पहाड़ियों के ऊपर बने छोटे छोटे गाँव। ये सभी आपस में मिलकर एक ऐसा अप्रतिम दृश्य प्रस्तुत करते हैं मानो लद्दाख के बीहड़ पर्वतीय क्षेत्र में एक रमणीय स्थल प्रस्फुटित हो गया हो। हमें यह जानकार सुखद आश्चर्य हुआ कि इन बीहड़ पर्वतीय ढलानों में वृक्षारोपण के पावन उपक्रम का शुभ आरम्भ मठ के दृप्काओं ने ही किया है।
हेमिस मठ का नरोपा उत्सव
हमने हेमिस मठ का भ्रमण नरोपा उत्सव के समय ही किया था। हमें इस उत्सव में कुछ दिवस भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। सत्य कहूं तो यदि आप इस क्षेत्र की संस्कृति एवं परम्पराओं को जानना व समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ के एक नहीं, अनेक भ्रमण करने पड़ेंगे। विश्वास कीजिये, आपका प्रत्येक भ्रमण आपको नित नवीन ज्ञान प्रदान करेगा तथा संतोषप्रद अनुभव प्रमाणित होगा।

महामार्ग से यह मठ एक तीन तल की संरचना प्रतीत होती है। पहाड़ी की तलहटी से सिन्धु नदी बहती है जिसके तट के निकट से एक सर्पिल मार्ग मठ के प्रवेश द्वार तक जाता है। मार्ग के एक ओर एक नवनिर्मित शुभ्र श्वेत नरोपा स्तूप है जिसका नाम नारो फोतांग है। उसे लकड़ी के उत्कीर्णित सजावटों से अलंकृत किया गया है। नरोपा उत्सव यहीं आयिजित किया जाता है।
इसी सर्पिल मार्ग द्वारा कुछ किलोमीटर आगे जाने पर आप एक सुन्दर मठ पर पहुंचेंगे जिसे मिट्टी की ईंटों द्वारा निर्मित किया गया है। इस मठ से पुरातनता स्पष्ट झलकती है तथा इसकी पुरातनता को बनाए रखने का पर्याप्त प्रयास भी किया गया है।
दृप्का का हेमिस मठ
दृप्का वंशावली के अंतर्गत तिब्बती बौद्ध धर्म के एक विशेष धार्मिक पंथ का पालन करने वाला यह हेमिस मठ पुरातनता के मापदंड में अनेक वर्ष प्राचीन है। वर्ष १६७२ में लद्दाखी सम्राट सेंग्गे नाम्ग्याल ने इस मठ को पुनर्जीवित कर इसे इसका प्राचीन गौरव पुनः प्रदान किया था। यह तांत्रिक बौद्ध मान्यताओं के प्रमुख स्थानों में से एक है। ऐसी मिथ्याएं हैं कि जीसस क्राइस्ट ने अपने पूर्वोत्तर भ्रमण के अंतिम कुछ दिवस इस मठ में व्यतीत किये थे।

गोम्पा के रहस्यमयी मुखौटा नृत्य, प्राचीन पांडुलिपियाँ, हस्तचित्रित भित्तिचित्र, धुपबत्ती आदि इसके रहस्यमयी भूतकाल की कथाएं कहते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है, इस मठ को लद्दाख क्षेत्र के सर्वाधिक संपन्न बौद्ध मठों में से एक माना जाता है। इस मठ का मुख्य संकुल एक दो-तल की संरचना है जिसे ठेठ लद्दाखी निर्माण शैली में निर्मित किया गया है, अर्थात् मिट्टी की इंटों द्वारा निर्मित भित्तियों पर काष्ठकारी द्वारा अलंकरण, भित्तियों पर पुते पीले व लाल रंग जो बौद्ध भिक्षुओं के परिधान के रंग होते हैं, आदि।
और पढ़ें: लद्दाख के स्पितुक बौद्ध मठ का रहस्यमयी चाम नृत्य
आप यहाँ दीप कक्ष का अवलोकन करना ना भूलें। इस कक्ष में विभिन्न आकारों के दीपों में याक का मक्खन डालकर दीप प्रज्ज्वलित किया जाता है। उनमें से कुछ वर्ष भर प्रज्ज्वलित रहते हैं तथा कुछ दीपों को केवल एक रात्रि के लिए प्रज्ज्वलित रखा जाता था। इन दीपों को मृत बौद्ध भिक्षुओं की स्मृतियाँ अथवा पावन आत्मा माना जाता है। मठ में आये भेंटकर्ता तीनों गोम्पा के भीतर जा सकते हैं तथा बुद्ध के विभिन्न रूपों एवं उनके शिष्यों की आराधना करते भिक्षुओं के दर्शन कर सकते हैं। बुद्ध के विभिन्न रूपों की प्रतिमाओं में सर्वाधिक भव्य है, गुरु पद्मसंभव की प्रतिमा। बौद्ध धर्म के तिब्बती विद्यालयों के अनुसार गुरु पद्मसंभव को प्रसिद्ध ‘बुद्ध द्वितीय’ माना जाता है।
मठ के विस्तृत प्रांगण का प्रयोग प्रसिद्ध हेमिस त्सेचू उत्सव का आयोजन करने के लिए भी किया जाता है। यह उत्सव तिब्बती पंचांग के त्से-चू चन्द्र-मास में गुरु पद्मसंभव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है।
संग्रहालय
प्रांगण के दूसरे छोर पर उत्कृष्ट हेमिस संग्रहालय है। इस संग्रहालय का आकार इतना छोटा था कि मुझे इसके संग्रहों की व्यापकता पर आशंका उत्पन्न होने लगी थी। किन्तु मेरी आशंकाओं के विपरीत यह संग्रहालय अत्यंत ही समृद्ध सिद्ध हुआ। इस छोटे से संग्रहालय में असंख्य बौद्ध अवशेष, कलाकृतियाँ तथा ऐतिहासिक प्रलेखन प्रदर्शित हैं। इस संग्रहालय के अवलोकन का अनुभव ऐसा था मानो हम इस मठ के सभ्यता के अभ्युदय से लेकर वर्तमान तक के इतिहास को जीवंत अनुभव कर रहे हों।

यहाँ गांधार शैली की प्रतिमाएं हैं जो सिकंदर के कालखंड से सम्बन्ध रखती हैं, तो साथ ही त्से-चू उत्सव का श्वेत-श्याम चित्र भी है। एक ओर वयस्क हिम तेंदुए की चमड़ी लटकी हुई है, जिनका प्राचीन काल में ध्यान साधना में बैठने के लिए चटाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। वहीं संग्रहालय की भित्तियाँ रक्षक मुखौटों से पूर्णतः सज्जित हैं।
हेमिस संग्रहालय की अधिकतर कलाकृतियों का विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। उन कलाकृतियों को यहाँ दक्षता से सहेज कर रखा जाता है तथा प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि ऐतिहासिक व पुरातात्विक दृष्टि से ये अनमोल हैं। संग्रहालय के भीतर छायाचित्रीकरण की अनुमति नहीं है।
नरोपा उत्सव
इस उत्सव की अपार महत्ता है। यहाँ तक कि इसे हिमालय का कुम्भ मेला कहा जाता है। किसी भी अन्य कुम्भ मेले के समान इस उत्सव में भी विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। ऊँचे पर्वत की ढलुआ चढ़ाई चढ़कर मठ तक पहुँचते हैं।
पवित्र अवशेष
बौद्ध शात्रज्ञ नरोपा की अस्थियाँ एवं केशों से निर्मित आभूषणों को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए बाहर निकाला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अस्थि अवशेषों से निर्मित छः आभूषण डाकिनी का वरदान हैं। वे हैं, मुकुट, गले का हार, कान के कुंडल, कंगन, सेरल्खा तथा तहबन्द। इन पावन अवशेषों को लेकर एक भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है जो हेमिस मठ से आरम्भ होकर नारो फोतांग नरोपा स्तूप के प्रांगन में समाप्त होती है।

परंपरा के अनुसार इन आभूषणों को महामहिम ग्यालवांग दृप्का धारण करते हैं जो Live to Love initiative के संस्थापक भी हैं। यह संस्था वहां के रहवासियों के जीवन में धार्मिक परम्पराओं की परिसीमा से परे जाकर सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करती है।

इस उत्सव में भव्य प्रदर्शन करने के लिए लद्धाख के दूरस्थ भागों की जनजातियाँ अनेक दिवसों तक अभ्यास करती हैं। पारंपरिक लद्दाखी परिधानों तथा मस्तक के पारंपरिक मुकुटों को संदूकों से बाहर निकला जाता है। स्वयंसेवकों द्वारा इस क्षेत्र के पारम्परिक व्यंजन बनाये तथा सभी को प्रस्तुत किये जाते हैं। उनमें पर्वतीय कुकुरमुत्ते, स्थानीय पालक तथा अन्य हरी भाजियां प्रमुख हैं। किन्तु सर्वाधिक विशेष है, याक के दूध का स्वादिष्ट चक्का या चीस।
और पढ़ें: शाकाहारियों के लिए लद्दाख यात्रा
वार्षिक नरोपा उत्सव
पूर्व के रीति-रिवाजों के अनुसार यह उत्सव बारह वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता था। किन्तु लद्दाख में प्रतिदिन बढ़ते पर्यटकों को देखते हुए वहां के अधिकारियों ने इसे वार्षिक उत्सव में परिवर्तित करने का निश्चय किया। उनकी यह पहल सराहनीय है क्योंकि इससे वहां के लोगों को बढ़ते पर्यटन का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। वहीं, पर्यटकों को लद्दाख की परम्पराओं एवं संस्कृति को जानने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। लद्दाख को भी पांगोंग सरोवर तथा चादर ट्रेक के परे जाकर एक विशिष्ट पहचान प्राप्त हो रही है।

हमने दूर से पारंपरिक लद्दाखी परिधान धारण कर लकड़ी की सहायता से चलते हुए स्थानीय लोगों को देखा। अपनी माताओं की गोद से झांकते हुए गुलाबी गुलाबी गालों वाले नन्हे हमें उत्सुकता से देख रहे थे। ना हमें लद्दाखी भाषा आती थी, ना ही हिन्दी में उनकी निपुणता थी। टूटी-फूटी हिन्दी ही हमारे मध्य के भाषा व्यवधान को मिटा रही थी।
हमने सम्पूर्ण उत्सव तथा सभी प्रदर्शनों को देखा। लद्दाखी नानी-दादियों ने हमें उनके बागीचों से तोड़े ताजे सेब खिलाये। यह स्थान अब भी अत्यधिक पर्यटन अतिक्रमण से मुक्त है। इसी कारण पर्यटकों एवं स्थानिकों के मध्य सम्बन्ध अब भी अत्यंत मधुर हैं। उनके आचरण पर पर्यटन संबंधी व्यापारिक लेनदेन की छाया भी नहीं पड़ी है। अन्य पर्यटन स्थलों के विपरीत यहाँ प्लास्टिक की पोतियाँ, कागज की वस्तुएं तथा अन्य अजैवनिघ्नीकरणीय कचरे ने निर्मल पर्वतों को अपवित्र नहीं किया है। इसके लिए हमें दृप्काओं का आभार मानना चाहिए।

किन्तु एक सत्य यह भी है कि उत्सव काल में, रात्रि के समय लद्दाख को बॉलीवुड प्रफुल्लित कर देता है। यूँ तो भारतीय उप-महाद्वीप पर भारतीय चित्रपट व्यवसाय का प्रभाव अभूतपूर्व है। किन्तु उसने अपनी लोकप्रियता के द्वारा अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। मैंने ऐसे अनेक पर्यटकों के देखा जो पांगोंग सरोवर से लेह की ओर जाते समय इस उत्सव में भाग लेने के लिए यहाँ स्वैच्छिक रूप से तत्क्षण रुक गए जब कैलाश खेर, पापोंन तथा सोनू निगम जैसे जगप्रसिद्ध गायकेरस्तुत करने के लिए तत्पर हो गए. इस उत्सव में उनके पसंदीदा गीतों को प्रस्तुत करने लगे। भारतीय सेना के काफिले भी उत्साहपूर्वक उत्सव में भाग ले रहे थे। सम्पूर्ण वातावरण अत्यंत उत्साहवर्धक तथा आनंदपूर्ण हो गया था। संगीत विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एक सूत्र में बांधने का सफल साधन होता है। जनवरी मास में लद्दाख की शुष्क मरू क्षेत्र की जमा देने वाली ठण्ड में भी किसी के उत्साह में तनिक भर भी कमी नहीं आयी थी।
७० फीट लम्बी हस्त-चित्रित थान्ग्का चित्र
नरोपा उत्सव के दूसरे दिवस ७० फीट लम्बी एक हस्त-चित्रित थान्ग्का चित्र को प्रदर्शित किया गया था। वहां उपस्थित सभी लोग झुक कर उसे प्रणाम कर रहे थे। उस चित्र में अमिताभ बुद्ध के आठ विभिन्न रूप चित्रित थे। इस चित्र को केवल कुछ घंटों के लिए ही बाहर निकालकर फहराया जाता है। तत्पश्चात इस ऐतिहासिक वस्त्र को उतारकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है ताकि सूर्य के प्रकाश में इसके रंगों को कोई हानि ना पहुंचे।

लद्दाखी संस्कृति एवं परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदहारण प्रस्तुत किया तीन सौ लद्दाखी स्त्रियों ने, जिन्होंने “शोंडोल” नामक नृत्य का प्रदर्शन किया। यह नृत्य उत्सव के समापन के दिन किया जाता है। लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाने जाने वाले इस शोंडोल नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में प्रवेश करके इतिहास रच दिया है। पर्वतों के मध्य गूंजती ढोल की नाद-ध्वनी जो मैंने उस दिन सुनी, वह अब भी मेरे कानों में गूंजती है।
स्थानीय जीवन पर नरोपा उत्सव का प्रभाव
यूँ तो लद्दाख में अनेक सांस्कृतिक भव्य उत्सव आयोजित किये जाते हैं। उनमें लोसर महोत्सव एवं सिन्धु दर्शन प्रमुख हैं। लद्दाख के विभिन्न उत्सव वहां के आकर्षक चाम नृत्य के कारण अत्यंत लोकप्रिय हैं। इतने सुन्दर एवं भव्य महोत्सवों के पश्चात क्या आवश्यकता थी कि नरोपा उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाए? यह प्रश्न आपके मन में भी आया होगा!
नरोपा उत्सव का उद्देश्य है, दृप्का वंशावली द्वारा किये गए चिरस्थाई विकास प्रयासों के विषय में जागरूकता फैलाना। पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली से लेकर चिरकालीन यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने तक, ‘लीव टू लव’ संस्था सतत इस ओर प्रयासरत है ताकि स्थानिकों को शिक्षित किया जा सके तथा उनमें आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। यह उत्सव उनके इन्ही प्रयासों का साक्ष्य है।
सकारात्मक बदलाव का एक उदहारण है, नरोपा फेलोशिप। नवीन शैक्षणिक अधिछात्रवृत्ति अथवा फेलोशिप का उद्देश्य है, हिमालयीन क्षेत्रों के युवाओं को सक्षम करना। यह फेलोशिप विश्वभर में रहने वाले लाद्दखी मूल के लोगों के लिए उपलब्ध है। योग्यता छात्रवृत्ति के लिए छात्रों के प्रथम समूह का चयन किया जा चुका है। इस उपक्रम का ध्येय है, इस शुष्क क्षेत्र के अतिसंवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले स्थानिकों की जीविका के साधनों को सुगम व चिरस्थाई बनाना।
उत्सव काल में मठ का भ्रमण स्वयं में एक अद्वितीय अनुभव है। एक अविस्मरणीय अनुभव! सभी संवेदनशील पर्यटक जिन्हें सांस्कृतिक अनुभवों के लिए सम्मान है, इस मठ की यात्रा तथा उत्सव में भाग लेने के अनुभवों को अपनी स्मृतियों में सदा जीवित रखेंगे।
यह संस्करण मधुरिमा चक्रवर्ती ने लिखा है जिन्होंने लद्दाख के नरोपा उत्सव में इंडीटेल्स का प्रतिनिधित्व किया था।
मधुरिमा कोलकाता में जन्मी, बैंगलोर में स्थाई तथा Orangewayfarer नामक यात्रा ब्लॉग की संस्थापक हैं। उन्हें खाना, साड़ियाँ, पुस्तकें, छायाचित्रीकरण तथा पर्यावरण अनुकूल यात्राएं करना प्रिय है। उनका स्वप्न है कि वे भविष्य में अंटार्टिका की यात्रा अवश्य करेंगी।