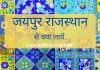नेपाल की थारु जनजाति से मेरा प्रथम साक्षात्कार तब हुआ जब मैं नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित बरही जंगल लॉज में उनके द्वारा आयोजित नृत्य प्रदर्शन का आनंद ले रही थी। हम नेपाल यात्रा के इस पड़ाव में बरही जंगल लॉज में ठहरे थे। वहाँ पहुँचने के लिए हम वायुमार्ग द्वारा नेपाल के भरतपुर विमानतल पर पहुँचे थे। मेरे अनुभव में आया वह तब तक का सबसे लघु आकार का विमानतल था।

हम वहाँ से बरही जंगल लॉज पहुँचे। हमारे पहुँचने तक सूर्यास्त हो चुका था। लॉज में आगमन की औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात हम राप्ती नदी के तट पर बैठ गए। रात्रि के मंद प्रकाश में राप्ती नदी लगभग अदृश्य प्रतीत हो रही थी।
थारु जनजाति – नृत्य एवं संगीत
लॉज के कर्मचारी शिविराग्नि जलाने में व्यस्त हो गए थे। नृत्य एवं संगीत प्रदर्शन के लिए कलाकार प्रस्तुत होने लगे थे। सभी कलाकारों ने श्वेत-श्याम परिधान धारण किया हुआ था। मुझे उनके परिधान कुछ असामान्य प्रतीत हुए। मेरा यात्रा अनुभव यह कहता है कि हम किसी भी क्षेत्र के जितना भीतर जाते हैं, वहाँ के निवासियों के परिधान उतने ही विविध रंगों से परिपूर्ण होते जाते हैं। सम्पूर्ण प्रदर्शन दल के परिधानों में श्वेत-श्याम के अतिरिक्त कोई भी अन्य रंग उपस्थित नहीं था। केवल कमरपट्टे से रंगीन वस्त्र का एक छोटा टुकड़ा लटक रहा था तथा केश में लाल फीते थे। स्त्रियों ने सिक्कों का आभूषण धारण किया था। कहा जाता है कि सम्पूर्ण विश्व के सभी जनजाति क्षेत्रों की स्त्रियों में सिक्कों के आभूषण सामान्य हैं।

प्रदर्शन दल ने अग्नि के चारों ओर नृत्य करना आरंभ किया। पुरुष कलाकारों का एक दल संगीत वाद्य बजा रहा था। वयोवृद्ध स्त्रियों का एक समूह एक पंक्ति में खड़े होकर गीत गा रहा था। अन्य सभी कलाकार नृत्य करने लगे जिसमें वे डंडियों का भी प्रयोग कर रहे थे। मैंने वहाँ नेपाल का सर्वाधिक लोकप्रिय लोकगीत सीखा, रेशम फिरीरी। उन्होंने मुझे बताया कि यदि मैं इस गीत को भूल भी जाऊँ तो पुनः स्मरण करने के लिए यूट्यूब की सहायता लूँ। यह गीत यूट्यूब पर उपलब्ध है।
उन्होंने एक युद्ध नृत्य प्रस्तुत किया जिसे बजेति कहते हैं। आप इस नृत्य में वीर रस स्पष्ट देख सकते हैं। उन्होंने डम्फु नृत्य प्रस्तुत किया जो सामान्यतः होली के पर्व पर किया जाता है। इस नृत्य में होली का उल्हास स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। तत्पश्चात उन्होंने ठाकरा नृत्य किया जिसमें उन्होंने डांडिया सदृश डंडियों का प्रयोग किया। यह नृत्य भरपूर फसल का उत्सव मनाता है।

झमता नृत्य में केवल स्त्रियाँ ही भाग लेती हैं। मुझे वह लोकगीत एवं नृत्य कुछ चंचल प्रतीत हुआ। अतः मुझमें उस लोकगीत का अर्थ जानने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। नृत्य प्रदर्शन के समाप्त होते ही मैंने एक वयस्क गायिका स्त्री से गीत का अर्थ पूछा। उन्होंने स्मित हास्य पर विषय को टाल दिया। मैंने देखा, उनके हाथों में सघनता से गोदना गुदा हुआ था। उन्होंने हमें बताया कि विवाह के समय उन्होंने वह गोदना गुदवाया था।

मुझे थारु जनजाति के कलाकारों द्वारा प्रदर्शित गीत एवं नृत्य अत्यंत लुभावने प्रतीत हुए। मुझमें उनके गाँव का अवलोकन करने एवं उनकी जीवनशैली को जानने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हुई। मैंने चितवन राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित थारु गाँवों के दर्शन करने का निश्चय किया।
नेपाल की थारु जनजाति
बरही जंगल लॉज में स्थित पुस्तकालय में मैंने नेपाल की थारु जनजाति पर प्रकाशित एक लघु पुस्तिका पढ़ी। उसके अनुसार थारु जनजाति की वंशावली आंशिक रूप से राजस्थान के थार मरुभूमि के राजपूत वंश की ओर संकेत करती है। कहा जाता है कि इस जनजाति के पुरुष नेपाली हैं तथा स्त्रियाँ राजस्थानी मूल की हैं। ऐसा भी माना जाता है कि चूंकि स्त्रियों ने अपने से निम्न जाति के पुरुषों से विवाह किया था, अतः परिवार में उनका वर्चस्व होता है। स्त्रियों को संपत्ति पर विशेषाधिकार भी होता है। कुछ ग्रंथों में इतना भी लिखा था कि स्त्रियाँ भोजन की थालियाँ पुरुषों की ओर अपने पैर से ढकेलती हैं। मैंने इस तथ्य की पुष्टि करने के उद्देश्य से कुछ स्त्रियों से इस विषय पर चर्चा की किन्तु किसी ने भी इस तथ्य की पुष्टि नहीं की।
इस पुस्तिका में इस जनजाति के विषय में आँकड़े प्रकाशित किये गए थे। भारत-नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों निवास करते थारु जनजाति की जीवनशैली के विषय में वर्णन किया गया था।
थारु जनजाति मलेरिया रोग से प्रतिरक्षित है – शोध के अनुसार उनके विशेष वंशाणु उन्हे मलेरिया रोग के प्रति रोधक क्षमता प्रदान करते हैं।
थारु जनजाति स्वयं को वनवासी मानती है। उनके गाँव सामान्यतः वन के भीतर स्थित होते हैं। अतः वे वनों के भीतर तथा वनों की संगति में निवास करते हैं। वे आंशिक रूप से कृषि तथा आंशिक रूप से वनोपज पर निर्भर रहते हैं।

प्रत्येक गाँव का एक मुखिया होता है जिसे प्रत्येक वर्ष माघ मास में लोकतांत्रिक रूप से चुना जाता है। इस चुनाव के लिए मतदान का अधिकार एक परिवार को समग्र रूप से प्राप्त होता है, ना कि परिवार के प्रत्येक सदस्य अथवा वयस्क को। मुखिया को बड़घर कहा जाता है। उसके ऊपर गाँव के समग्र जनहित का उत्तरदायित्व होता है। उसे दोषी व्यक्ति को दंडित करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। गाँव के धार्मिक मुखिया का चुनाव भी इसी रीति से किया जाता है।
थारु जनजाति की बोलचाल भाषा थारु है जो कुछ सीमा तक हिन्दी, अवधि एवं मैथिली से साम्य रखती है।
अधिकांश थारु जनजाति हिन्दू धर्म का पालन करती है जबकि कुछ थारु मूलनिवासियों ने अब ईसाई धर्म अपना लिया है।
थारु सांस्कृतिक संग्रहालय, मेघौली
मेघौली गाँव में स्थित थारु सांस्कृतिक संग्रहालय वास्तव में एक कुटिया सदृश संरचना है। उसकी भित्तियों पर हल्के हरे रंग का रोगन किया हुआ था। उस पर हस्तछाप रंगे हुए थे। चितवन में भ्रमण करते हुए भी हमने मिट्टी के ऐसे अनेक कच्चे घर देखे जिनकी भित्तियों एवं द्वारों पर हाथों से विविध चिन्ह रंगे हुए थे।

यह एक एकल-कक्ष संग्रहालय है जहाँ थारु जीवनशैली को प्रदर्शित किया गया है। उनकी आजीविका के साधन, उनके नृत्य, उनकी परम्पराएं तथा उनके दैनंदिनी जीवन के दृश्य प्रदर्शित किये गए थे। वहाँ से मुझे इस तथ्य की पुष्टि हुई कि वे सदा श्वेत-श्याम परिधान धारण करते हैं, यहाँ तक कि अपने विवाह समारोह में भी। विविध चित्रों के माध्यम से थारु जनजाति के एक व्यक्ति के जन्म संस्कारों से लेकर मृत्यु संस्कारों तक की यात्रा का सुंदर चित्रण किया गया है जिनमें उसका विवाह संस्कार भी सम्मिलित है।
मेरी अभिलाषा है कि इस संग्रहालय में इस जनजाति का विस्तृत वर्णन करती अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
थारु जनजाति के निवासस्थान का भ्रमण
पारंपरिक थारु जनजाति के निवासस्थानों को एक अनूठे रूप से संयोजित किया जाता है। एक मुक्ताकाश प्रांगण के चारों ओर आवासों का एक समूह होता है। इस प्रकार सभी आवास स्वयं में स्वतंत्र होते हुए भी एक लघु समुदाय का भाग होते हैं। यह लघु समुदाय उनके परिवार से संबंधित अन्य परिवार भी हो सकते हैं।

मध्यस्थल में काष्ठ के ऊँचे पंछीघर होते हैं। प्रत्येक आवास के पार्श्वभाग में एक गौशाला होती है। उनकी इस संरचना से ऐसा आभास होता है मानो उनका आवास मानव, पंछियों एवं मवेशियों के मध्य बँटा होता है।

हमें थारु जनजाति के एक निवासस्थल का भीतर से अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ। परिवार की प्रमुख स्त्री ने द्वार पर खड़े होकर आरती की थाली से हमारा स्वागत किया। उसके चारों ओर द्वार पर तथा भित्तियों पर हाथों से सुंदर आकृतियाँ रंगी हुई थीं। एक क्षण के लिए मुझे यह सज्जा उसकी आभामंडल प्रतीत हुई। उन्होंने हमें अपना आवास दिखाया।

अपने पारंपरिक आभूषण दिखाए। आवास में रखे सभी संदूकों एवं भंडारण द्वारों पर भी वैसी ही हस्त निर्मित आकृतियाँ बनी हुई थीं।
थारु जनजातियों द्वारा हस्तछाप
मैंने यहाँ जिनसे भी भेंट की, उन सभी से इन हस्ताकृतियों का महत्व जानने का प्रयास किया। सभी ने यही कहा कि यह उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग है। वे सदा से ऐसी आकृतियाँ अपनी संरचनाओं पर चित्रित करते आ रहे हैं। मैंने अनुमान लगाया कि कदाचित ये शुभ चिन्ह हैं। इन चिन्हों ने मुझे उन हस्ताकृतियों का स्मरण कर दिया था जिन्हे मैंने राजस्थान में देखा था, जैसे जैसलमेर का सोनार किला अथवा बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। कदाचित यह एक ऐसा सांस्कृतिक सूत है जो उन्हे अब भी राजस्थान से बांधे हुए है।

आवास का अवलोकन करते हुए हम उसके पिछवाड़े में पहुँच गए। वहाँ बैठकर हमने परिवार के सदस्यों से कुछ क्षण वार्तालाप किया। उन्होंने हमारे समक्ष रोक्सी नामक पेय प्रस्तुत किया। यह एक स्थानीय पेय है जिसे किण्वित भात से बनाया जाता है। मुझे बताया गया कि यह एक प्रबल मदिरा है। मैंने उससे दूर रहना उत्तम जाना। उन्होंने कहा कि वे इस घरेलू पेय का नियमित सेवन करते हैं।
इस परिवार के सदस्यों ने मुझे अत्यंत आत्मीयता का अनुभव कराया। आवास से बाहर आते हुए मुझे ऐसा आभास हुआ मानो जिस संस्कृति को मैंने तीन दिवसों पूर्व ही जाना था, उस संस्कृति को अब कुछ कुछ समझने लगी हूँ।
उनके आत्मीयता से ओतप्रोत व्यवहार तथा हंसमुख मुखड़ों की स्मृतियाँ मेरी चितवन राष्ट्रीय उद्यान यात्रा की सर्वाधिक प्रिय स्मृति के रूप में सदा मेरे साथ रहेंगी।