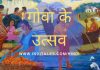कोणार्क सूर्य मंदिर विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। इसके वर्तमान स्वरूप को देखकर इसकी प्राचीन काल की भव्यता एवं शोभा की कल्पना करना असंभव ना सही, कठिन अवश्य है। जब यह अखंडित मंदिर अपने सम्पूर्ण वैभव में अस्तित्व में था तथा इसके सातों घोड़े ऐसे प्रतीत होते थे मानों सूर्य के विशाल रथ को लेकर हवा से बातें कर रहे हों। इस मंदिर की विशालता एवं भव्यता का यदि थोड़ा सा आभास कोई दे सकता है तो वह है पुरी का जगन्नाथ मंदिर।

ओडिशा में ४ विभिन्न क्षेत्र हैं। इन्हे उन ४ वस्तुओं से जाना जाता है जिन्हे भगवान विष्णु अपने चार हाथों में धारण करते हैं। उनमें से एक पद्म अर्थात कमल है। कोणार्क को पद्म क्षेत्र कहा जाता है। वस्तुतः एक समय कोणार्क सूर्य मंदिर को पद्मकेसर देऊल कहा जाता था तथा मंदिर के अधिष्ठात्र सूर्य देव, महाभास्कर के नाम से जाने जाते थे। कोणार्क उन कोने को दर्शाता है जहां सूर्य देव अर्थात आदित्य की आराधना की जाती है। इस क्षेत्र को अर्क क्षेत्र भी कहते हैं।
कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास
पौराणिक सूत्रों के अनुसार उत्कल की चंद्रभागा नदी का तट सूर्य की आराधना का स्थल था। उत्कल ओडिशा का ही प्राचीन नाम है। किवदंतियों में कृष्ण एवं जांबवती के पुत्र सांब से इस स्थान का संबंध प्राप्त होता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार सांब ने अपनी किसी त्वचा विकार से मुक्ति पाने के लिए यहीं सूर्य की उपासना की थी। इस स्थान का संबंध मुल्तान से भी जोड़ा जाता है जो किसी समय सूर्य उपासना का प्रमुख केंद्र था। यदि आपको स्मरण हो तो चिनाब नदी को भी चंद्रभागा कहा जाता है क्योंकि यह चंद्रा एवं भागा इन दो नदियों के संगम से अस्तित्व में आई है।

ज्ञात ऐतिहासिक सूत्रों की चर्चा की जाए तो स्थानीय तालपत्र पांडुलिपियों से हमें जानकारी मिलती है कि प्रारंभ में केसरी वंश के राजाओं ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। तत्पश्चात गंगा वंश के राजाओं ने इस मंदिर में पूजा अर्चना जारी रखी। १३ वीं. सदी में राजा नरसिंहदेव ने पुराने मंदिर के समक्ष इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के निर्माण में १२ वर्षों का समय लगा। इस पर प्रथम आक्रमण १६ वीं. सदी के मध्य में हुआ जब आक्रमणकारी मंदिर का कलश एवं ध्वज ले जाने में सफल हुए।
चैतन्य महाप्रभु एवं अबू फजल उन प्रसिद्ध यात्रियों में से हैं जिन्होंने इस मंदिर के दर्शन किए थे।
और पढ़ें: मोढेरा सूर्य मंदिर – अद्वितीय वास्तुशिल्प का उदाहरण
पतन
इस मंदिर के पतन के विषय में अनेक धारणाएं हैं। काला पहाड़ जैसे आक्रमणकारी के हाथों ध्वस्त होने से लेकर अभियांत्रिकी असफलता तक, जो इसके क्रमशः विनाश का कारण बनी। १९ वीं. सदी में जेम्स फर्गुसन ने जब इस मंदिर को देखा था तब यह मलबे का एक ढेर था तथा यहाँ से कोई भी प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई थी। १८ वीं. सदी में इस मंदिर के प्रमुख स्तंभ, अरुण स्तंभ को मराठा शासकों ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थानांतरित कर दिया था। आज आप यहाँ महामंडप का केवल आवरण देखेंगे जिसके भीतर रेत भरी हुई है। इसके समक्ष नाट्य मंडप है। सौभाग्य से इस की भित्तियों को संरक्षित रखा गया है। आप इनके ऊपर की गई शिल्पकारी के अवलोकन का आनंद उठा सकते हैं।

ऐसी मान्यता है कि मुख्य सूर्य प्रतिमा चुंबकीय बलों के संतुलन द्वारा मंदिर के मधोमध हवा में लटकी हुई थी। प्रतिदिन सूर्योदय की प्रथम किरण मूर्ति के माथे पर पड़ती थी जो सूर्योदय का प्रतीक थी।
इस मंदिर के दर्शन करते समय आप इन महत्वपूर्ण तत्वों के दर्शन करना ना भूलें।
कोणार्क सूर्य मंदिर के २४ महत्वपूर्ण तत्व
१ विशाल वास्तुशिल्प
कोणार्क सूर्य मंदिर कलिंग मंदिर-वास्तुशिल्प का अप्रतिम उदाहरण है जिसके दर्शन विरले हैं। मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि वास्तुकार की कल्पनाशक्ति कितनी अपरंपार होगी जो उसने ७ घोड़ों द्वारा हाँके जाते एक भव्य रथ के रूप में एक मंदिर की कल्पना की होगी। ७ घोड़ों के रथ पर सवार सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर का इससे उत्तम स्वरूप नहीं हो सकता।

जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है, मंदिर का ऊपरी भाग, अर्थात कलश व ध्वज, अब अनुपस्थित है। फिर भी यह मंदिर अत्यंत विशाल प्रतीत होता है। रथ में २४ चक्र अथवा पहिये हैं जो दिन के २४ घंटों की ओर संकेत करते हैं। कुछ का मानना है कि ये वर्ष के २४ पक्षों से संबंध रखते हैं। रथ हाँकते ७ घोड़े सप्ताह के ७ दिवसों का प्रतीक हैं। सोचती हूँ कि उस समय यदि ऊपर से ड्रोन द्वारा छायाचित्रिकारण की सुविधा होती तो एक पूर्णतः निर्मित मंदिर की अप्रतिम वास्तु का उत्तम उदाहरण हमारे पास होता। एक रथ के आकार का होते हुए भी कलिंग देउल वास्तु शैली के सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं।
२. जगमोहन अथवा मंडप
मंदिर की जो विशाल संरचना हम देखते हैं वह इसका मंडप या अग्रशाला है जिसे ओडिशा में जगमोहन कहते हैं। इसके द्वार के चौखट पर अप्रतिम नक्काशी की गई है। मंडप की क्षीण संरचना पर चढ़ने अथवा इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ वर्जित है। आप फिर भी हरे रंग के चौखट देख सकते हैं जहां क्लोराइट शिला पर सूक्ष्म नक्काशी की गई है। शेष संरचना में खोंडालाइट एवं लेटराइट शिलाओं का प्रयोग किया गया है। इनमें से कोई भी शिला स्थानीय नहीं है। इन्हे कदाचित दूर-सुदूर स्थानों से चंद्रभागा नदी के जलमार्ग द्वारा आयात किया गया था।

शोधकर्ताओं के अनुसार इन शिलाओं को निखारकर उन्हे मढा गया था, तत्पश्चात उन पर यथास्थान शिल्पकारी की गई थी। इन कठोर पत्थरों पर किसी भी प्रकार की शिल्पकारी के लिए आवश्यक कौशल के विषय में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा एवं लिखा है। मंडप के द्वार भी सूर्य की गति के अनुसार पंक्तिबद्ध हैं। विषुव के दिवसों में अग्रभाग एवं पृष्ठ भाग के द्वारों से सूर्य की प्रथम किरणें मंडप के भीतर पहुँचती है। वहीं उत्तरायण एवं दक्षिणायन के समय मंडप के दोनों ओर के द्वारों से सूर्य की प्रथम किरणें भीतर प्रवेश करती हैं।
३. कोणार्क सूर्य मंदिर के शिल्प
कोणार्क सूर्य मंदिर के विषय में कहा जाता है कि इसकी संरचना एक भीमकाय दैत्य के समान की गई थी तथा परिसज्जन जटिल नक्काशी युक्त आभूषणों के समान की गई थी। इस पर की गई शिल्पकारी को देख आपको ऐसा आभास होगा जैसे यह किसी कुशल सुनार के हाथों गड़ा गया हो। किसी भी अन्य मंदिर के समान कोणार्क सूर्य मंदिर के शिल्पों में भी देवी-देवताओं की प्रतिमाएं, मानव जीवन के विभिन्न दृश्य, राजसी जीवनशैली के चित्र, रत्यात्मक शिल्प, वनस्पति व जीव, वास्तु रूपांकन, अलंकारिक तत्व इत्यादि विभिन्न अनुपातों में उपस्थित हैं।
४. गज पट्टिका

मंदिर संरचना की आधार पट्टिका पर गजों की प्रतिमाएं हैं। उन्हे देख ऐसा आभास होता है मानो उन हाथियों ने सम्पूर्ण संरचना का भार अपनी पीठ पर उठाया हुआ है। इन शिल्पों में हाथियों के शावकों को ढूँढना ना भूलें।
५. नाग-नगिनियों की प्रतिमाएं

मंदिर की बाहरी भित्तियों पर अपनी दृष्टि-स्तर पर नाग-नागिनियों की अनेक प्रतिमाएं हैं। उनमें से अधिकतर की देह आधे मानव तथा आधे भुजंग की है। दक्षिणावर्त चलते हुए जैसे ही आप मंदिर के चारों ओर घूमेंगे आपकी दृष्टि इन शिल्पों पर अवश्य पड़ेगी। इन प्रतिमाओं के आसपास युद्धकला तथा घुड़सवारी में रत स्त्रियों की भी प्रतिमाएं हैं।
६. जिराफ की प्रतिमा

इन शिल्पों में सर्वाधिक अचंभा करने वाली प्रतिमा एक जिराफ सदृश पशु की है। जिराफ इस क्षेत्र का स्थानीय पशु नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो पशु इस क्षेत्र के नहीं थे, उनके विषय में भी यहाँ के लोगों को जानकारी थी। क्या यह इस तथ्य का संकेत है कि इस क्षेत्र का अफ्रीका से व्यापारिक संबंध था? कदाचित इसका उत्तर सकरात्मक है। कल्पना करिए, अफ्रीका का एक व्यापारी शिल्पकार को जिराफ के विषय में जानकारी देकर उससे जिराफ की प्रतिमा गढवा रहा है। कदाचित किसी अफ़ीकी व्यापारी ने इसे उपहार स्वरूप दिया हो।
और पढ़ें: खिद्रापुर का कोपेश्वर महादेव मंदिर
इस शिल्प के समीप राजा नरसिंहदेव तथा उनकी रानी सीतादेवी की प्रतिमाएं हैं। इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण किया था।
७. विशाल गज प्रतिमा
मंदिर की ओर आते समय आप विशालकाय हाथी की प्रतिमा को देखेंगे। हाथियों के कुछ शिल्प आप मंदिर के समीप एक पीठिका पर भी देख सकते हैं। इन प्रतिमाओं में क्रुद्ध हाथी शिकार को जकड़ रहा है। कदाचित किसी युद्ध में भाग लेने वाले हाथियों को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया हो।

मंदिर की ओर जाती सीढ़ियों पर एक शिल्प है जिसमें एक सिंह एक हाथी को कुचल रहा है। यह शक्ति का प्रतीक है। इन शिल्पों को देख कुछ विद्वानों ने प्रश्न किया है कि क्या इस मंदिर का निर्माण किसी युद्ध में प्राप्त सफलता के स्मृति में किया गया था? मेरे गाइड के तर्क के अनुसार अत्यधिक संपत्ति एवं शक्ति अर्जित किए मानवों को इस प्रकार प्रताड़ित किया जाता था।

८. मैथुन शिल्प

अधिकतर प्राचीन मंदिरों के समान इस मंदिर में भी अनेक शिल्प हैं जो मैथुन क्रीडा प्रदर्शित कर रहे हैं। इनमें रति क्रीडा में संलग्न प्रेमी युगलों की प्रतिमाएं हैं जिनमें कुछ समलैंगिक भी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की पुस्तक से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मंदिर के शिल्प भारतीय शास्त्रों में दर्शाये गए सभी ९ रसों को प्रदर्शित करते हैं। मैथुन शिल्प शृंगार रस के अंतर्गत आता है। किन्तु इन शिल्पों को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है कि अन्य रसों की अपेक्षा ये शिल्प अधिक ध्यानाकर्षित करते हैं।
कुछ मतों के अनुसार इनका संबंध उपासना के तांत्रिक पथ से है, ओडिशा में जिसका प्रमुख रूप से अभ्यास किया जाता है।
९. हरे क्लोराइट द्वारा निर्मित सूर्य प्रतिमाएँ

मंडप के ऊपर सम्पूर्ण भित्तियों पर हरे रंग के क्लोराइट शिलाओं द्वारा निर्मित आदित्य की अनेक प्रतिमाएं हैं। इनके रंग के कारण ये उठकर दिखाई देते हैं। कई वर्षों पूर्व जब मैं यहाँ आई थी हम इन प्रतिमाओं के समीप तक जा सकते थे। किन्तु अब हमें इनकी सुंदरता को दूर से ही देख कर संतुष्ट होना पड़ता है। कुछ प्रतिमाओं में घुटने तक के ऊंचे जूते देख आप अचंभित हुए बिना नहीं रहेंगे।
१०. रुपये के भारतीय मुद्रा नोट पर अंकित प्रसिद्ध चक्र

मंदिर की दक्षिणावर्त परिक्रमा करते समय जो छटवाँ चक्र आप देखेंगे उस चक्र ने एक समय २० रुपये के भारतीय मुद्रा नोट पर विराजमान होकर उसे सम्मानित किया था। अब उसी चक्र की छवि १० रुपये के भारतीय मुद्रा नोट पर अंकित है। यह चक्र पर्यटकों में अत्यंत प्रसिद्ध है। वे इस चक्र का, १० रुपये की मुद्रा नोट के साथ अथवा स्वयं के साथ, छायाचित्र लेने में अत्यंत आनंदित होते हैं।

इन चक्रों की विशेषता यह है कि ये मात्र सजावटी चक्र नहीं हैं। अपितु ये धूप घड़ियाँ हैं। प्रत्येक चक्र के मध्य एक उभरी हुई मूठ है। जब सूर्य की किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं तब इन मूठों की परछाईयों द्वारा स्थानीय समय की गणना की जा सकती है। प्रत्येक चक्र के ऊपर गहन सूक्ष्म शिल्पकारी की गई है जो किसी ना किसी कला शैली का अभिलेखन करती है। मुद्रा नोट पर जिस चक्र की छवि अंकित है उस चक्र पर एक शिकारी की जीवनी प्रदर्शित है। मेरा निवेदन है कि आप इन चक्रों की कला शैली को सूक्ष्मता से निहारें। इससे इन कलाकृतियों के साथ न्याय होगा तथा आपको भी सुखद आनंद प्राप्त होगा।
११. विदेशी प्रभाव
कोणार्क की प्रतिमाएं प्राचीन भारत के साम्राज्यों की वैश्विक प्रकृति का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन प्रतिमाओं में आप चीनी यात्रियों तथा व्यापारियों की प्रतिमाओं को उनकी विशेष मुखाकृतियों द्वारा पहचान सकते हैं। उनमें से एक को आप बंद होने वाली मेज पर चीनी व्यंजन, नूडल्स को चीनी चम्मच, चॉपस्टिक्स् के साथ खाते देख सकते हैं। लंबी टोपी वाले फारसियों को भो आप आसानी से पहचान सकते हैं।

इन दो प्रकार के शिल्पों को देख मैंने निष्कर्ष निकाला कि ये पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंधों की ओर संकेत करते हैं। पूर्वी समुद्रतट पर बसे होने के कारण यहाँ चीनी प्रभाव कुछ अधिक रहा होगा। हमारे गाइड ने हमें मँगोलिया तथा तिब्बत के वासियों की भी प्रतिमाएं दिखाई। उस के अनुमान से वे कदाचित धूप सेकने यहाँ आते थे। उसके अनुमान को स्वीकारना मेरे लिए कठिन था।
और पढ़ें: अजंता की चित्रकारियों को समझें
१२. रथ के घोड़े

घोड़ों की मूर्तियाँ सहसा दृष्टिगोचर नहीं होतीं। इसके लिए आपको मंदिर से किंचित दूर जाना पड़ेगा। दौड़ते घोड़े की इन प्रतिमाओं में से एक ओडिशा का राज्य चिन्ह है।
१३. नाट्य मंडप

नाट्य मंडप अनेक स्तंभों से भरा एक ऊंचा मंच है जिसका निर्माण नृत्य प्रदर्शनों के लिए किया गया था। यहाँ की प्रतिमाएं विशेषतः नृत्य भंगिमाओं, मुद्राओं तथा संगीत वाद्यों को समर्पित है। इन्हे देख किसी उत्सव के आनंद की भावना उत्पन्न होती है।
१४. लोहे की सलाखें
मंदिर के निर्माण में लोहे के शिकंजों एवं जोड़ों का प्रयोग किया गया है। मंडप के द्वारों के ऊपर भी आप शहतीर के रूप में लोहे का प्रयोग देख सकते हैं। इन्हे समीप से देखना चाहते हैं तो बाग में स्थित एक मंच पर रखे ऐसे शहतीरों का अवलोकन कर सकते हैं। इन धरोहरों को देख आप स्वयं जान जाएंगे कि भारत में धातु विज्ञान कितना प्राचीन है।
और पढ़ें: देखिये भारतीय वास्तुकला के सर्वोत्तम अभियांत्रिकी अचम्भे
१५. माया देवी मंदिर
सूर्य मंदिर के पृष्ठभाग में एक मंदिर है जो माया देवी को समर्पित माना जाता है। कुछ जानकार इसे सूर्य की पत्नी छाया देवी को समर्पित मानते हैं। यह मंदिर सूर्य मंदिर से भी अधिक प्राचीन है।
१६. भोग मंडप
मंदिर के एक ओर स्थित बाग में अनेक नालियाँ हैं जो एक पीठिका तक पहुँचती हैं। यह रसोईघर तथा भोजन क्षेत्र था जिसे भोग मंडप कहा जाता है। इसके आसपास दो कुएं भी हैं।
१७. नवग्रह मंदिर

सूर्य मंदिर के निकास द्वार से कुछ आगे जाकर आप एक नवगृह मंदिर देखेंगे जहां अब भी पूजा अर्चना की जाती है। काले पत्थर के एक बड़े फलक पर ९ ग्रहों की छवियाँ उकेरी गई हैं। यह फलक कोणार्क के प्रवेशद्वार का एक भाग था। कोणार्क मंदिर का यह इकलौता भाग है जिसकी अब भी आराधना की जाती है।
१८. कोणार्क सूर्य मंदिर क्षेत्र संग्रहालय
कोणार्क मंदिर परिसर में स्थित क्षेत्र संग्रहालय इस प्रकार के सर्वोत्तम संग्रहालयों में से एक है। यहाँ अपने जीवंत काल के मूल स्वरूप को पुनः सजीव करने का प्रयास किया गया है। इसके निर्माण के प्रत्येक चरण को क्रमशः पुनर्जीवित करते हुए भारत में सूर्य की आराधना की संकल्पना तथा योग में इसकी केन्द्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। ओडिशा हस्तकला तथा अन्य कलाक्षेत्रों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है।

अंत में एनिमेटेड फिल्म की सहायता से कोणार्क मंदिर की कथा प्रस्तुत की जाती है। मैंने सर्वप्रथम मंदिर के दर्शन किये, तत्पश्चात संग्रहालय का अवलोकन किया। जब सूर्य अपनी पूर्ण शक्ति से दमक रहा हो तो उस समय आप संग्रहालय के दर्शन कर सकते हैं। तदनुसार मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। संग्रहालय के लिए पृथक टिकट क्रय करने की आवश्यकता है।
१९. कोणार्क नृत्य उत्सव
कोणार्क मंदिर के नाट्य मंडप में प्रत्येक वर्ष फरवरी मास में वार्षिक नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह कोणार्क के सर्वाधिक लोकप्रिय उत्सवों में से एक है। मेरी इच्छा है कि किसी वर्ष मैं इस उत्सव में अवश्य भाग लूँ।
२०. विश्व विरासत स्थल
१९८४ में कोणार्क मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अंकित किया गया था जो इसे इस प्रकार के प्राचीनतम विरासत स्थलों में से एक बनाता है। इस विषय में उल्लेख यहाँ देखें।
२१. समुद्र तट पर स्थित रामचंडी मंदिर
समुद्र तट पर स्थित यह एक प्राचीन मंदिर है जो देवी रामचंडी को समर्पित है। वे अर्क क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। एक काल में उनका मंदिर उस स्थान पर था जहां अब सूर्य मंदिर स्थित है।

महाभारत महाकाव्य के अनुसार जब श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए श्री लंका की ओर जा रहे थे तब देवी रामचंडी ने रावण को हराने के लिए श्री राम का मार्गदर्शन किया था। यह एक छोटा किन्तु अत्यंत लोकप्रिय मंदिर है।
मंदिर में मैंने एक पट्टिका पर दश महाविद्याएँ उत्कीर्णित देखीं जो इस मंदिर का तांत्रिक आयाम उजागर करता है। इस मंदिर के चारों ओर अनेक छोटे मंदिर हैं जिनके मुख समुद्र की ओर हैं।
२२. चंद्रभागा जलकुंड

चंद्रभागा नदी यहाँ से बहती हुई समुद्र में जाकर मिलती थी। वर्तमान में इस नदी का प्रतिनिधित्व केवल एक छोटा सा जलकुंड करता है जिसका नाम भी नदी के नाम पर ही है। तीर्थयात्री अब भी इस कुंड के जल में पवित्र स्नान करते हैं। यह कुंड समुद्र तट तथा रामचंडी मंदिर के समीप स्थित है। आप चंद्रभागा मेले में भाग ले सकते हैं जो प्रति वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन आयोजित किया जाता है।
२३. समुद्र तट पर नौका सवारी
आप समुद्र तट पर सूर्योदय का आनंद उठा सकते हैं अथवा नौका सवारी कर सकते हैं।
२४. ओडिया संस्कृति तथा सूर्य मंदिर से संबंधित स्मारिकाएं

टिकट खिड़की से लेकर मंदिर के प्रवेश द्वार तक मार्ग के दोनों ओर अनेक दुकानें हैं। यहां से आप ओडिया कला व संस्कृति से ओतप्रोत विभिन्न कलाकृतियाँ क्रय कर सकते हैं जिनमें सूर्य मंदिर का लघु प्रतिरूप भी सम्मिलित है।
कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए यात्रा सुझाव
- कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी से ४० किलोमीटर तथा भुवनेश्वर से ६० किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ओडिशा के स्वर्ण त्रिभुज का एक भाग है।
- मंदिर के विस्तृत अवलोकन के लिए कम से कम २ घंटों का समय आवश्यक है। संग्रहालय दर्शन के लिए ३०-४० मिनटों का अतिरिक्त समय चाहिए।
- क्षेत्र संग्रहालय के समीप एक अच्छा जलपान गृह है जहां आपको अनेक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो जायेंगी। इनके अतिरिक्त नवगृह मंदिर के समीप भी अनेक ठेले तथा छोटी दुकानें हैं जहां से आप खाद्य पदार्थ क्रय कर सकते हैं।
- कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर में छायाचित्रिकारण वर्जित नहीं है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अधिकृत परिदर्शक अथवा गाइड यहाँ उपलब्ध हैं किन्तु मैं उनके ज्ञान से संतुष्ट नहीं हूँ। यदि संभव हो तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की कोणार्क पर जारी की गई मार्गदर्शक पुस्तिका ले लें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा विश्व विरसती स्थलों पर प्रकाशित श्रंखला का यह एक भाग है। कोणार्क के दर्शनीय स्थलों को स्वयं अवलोकन करते हुए इनके विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने का यह श्रेष्ठतर साधन है। मैं आशा करती हूँ कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अपने परिदर्शकों के प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान केंद्रित करे।
- कोणार्क सूर्य मंदिर मंदिर परिसर में आपको चलना पड़ता है। अतः अपने साथ पर्याप्त पेयजल तथा खाद्य पदार्थ अवश्य रखें।