उदयगिरी, रत्नागिरी एवं ललितगिरी ओडिशा में प्राचीन बौद्ध धर्म की अंतिम स्मृतियाँ हैं। इन स्थलों का संबंध बौद्ध धर्म के उदय से भले ही ना हो किन्तु बौद्ध धर्म के प्रसार में इनका निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान है।
ओडिशा में बौद्ध धर्म का इतिहास
ऐसी मान्यता है कि जब भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था तब उनके आरंभिक शिष्यों में दो शिष्य उत्कल अर्थात् ओडिशा के निवासी थे। उनके नाम थे, तपस्सु (तपुसा) तथा भल्लिका (बहलिका)।

ऐसा कहा जाता है कि २६१ ई.पू. में हुए कलिंग युद्ध के पश्चात ओडिशा (कलिंग) के सम्राट अशोक ने अहिंसा को अपनाया तथा पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में प्रवेश किया। समस्त विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार करना उनका लक्ष्य बन गया। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म का भारत से समस्त विश्व में प्रसार करने में सर्वाधिक योगदान सम्राट अशोक का ही था। भुवनेश्वर के समीप धौली में अशोक का स्तम्भ तथा उनके अनेक शिलालेख हैं।
कहते है कि सम्राट अशोक की सुपुत्री संघमित्रा ने यहीं से श्री लंका की यात्रा आरंभ की थी। वो श्रीलंका के अनुराधापुरा के समीप स्थित मिहिन्तले पहुंची थी। यह स्थान आज भी उसकी यात्रा का उत्सव मनाता है।
उदयगिरी, रत्नागिरी तथा मंगलगिरी, ये तीनों स्थल वास्तव में तीन विहार थे। बौद्ध धर्म में मठों या आश्रमों को विहार कहा जाता है। कदाचित इनका प्रयोग उस समय किया गया था जब इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर था। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने अपनी यात्रा विवरणों में कहा है कि ७ वी. शताब्दी में जब उसने इस स्थान की यात्रा की थी, तब भी ये तीनों विहार सक्रिय थे।
ओडिशा के हीरे- उदयगिरी, रत्नागिरी एवं ललितगिरी का विडिओ
हमारी उदयगिरी, रत्नागिरी एवं ललितगिरी की यात्रा के समय हमने यहाँ के प्रसिद्ध धरोहरों की झलक को आपके लिए अपने कैमरे में उतार लिया था। इन ऐतिहासिक धरोहरों को जानने एवं उचित परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए इस लघु चलचित्र को अवश्य देखिए।
तो आईए मेरे साथ इन विहारों एवं महाविहारों के दर्शन के लिए, जहां भिक्षु निवास करते थे तथा प्रार्थना एवं साधना करते थे।
उदयगिरी
तीनों ऐतिहासिक स्थलों में से विशालतम स्थल, उदयगिरी, बिरुपा नदी के किनारे स्थित है। बिरुपा नदी अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। इस स्थान को सन् १९५८ में उत्खनित किया गया था। सन् १९९७ में जब यहाँ पुनः खुदाई की गई तब यहाँ से कई स्तूप, मठ संकुल तथा बौद्ध विहार उत्खनित किये गए थे । उदयगिरी बौद्ध विहार का मूल नाम माधवपुरा महाविहार था। उदयगिरी, यह नाम यहाँ स्थित एक पर्वत के नाम से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है, उगते सूर्य का पर्वत।

ऐतिहासिक संरचनाओं से प्रथम साक्षात्कार के लिए आतुर, हम वृक्षों से घिरे एक पगडंडी से आगे बढ़े। हम जैसे ही समीप पहुंचे, बुद्ध एवं बोधिसत्व की आदमकद प्रतिमाओं से हमारा साक्षात्कार हुआ। ये प्रतिमाएं किंचित भंगित होने के पश्चात भी अत्यंत मनमोहक थीं। प्रतिमाओं का सूक्ष्म उत्कीर्णन देख हम अत्यंत रोमांचित थे। जब ऐसी प्रतिमाएं बाहर हैं तो अंदर कितनी अप्रतिम प्रतिमाएं होंगीं, इस विचार से हमारा रोम रोम प्रफुल्लित था।
उदयगिरी का बौद्ध विहार आरंभिक ईसवी से १३ वीं ई. तक सक्रिय था। निश्चित ही एक लंबे अंतराल तक यहाँ बौद्ध धर्म फल-फूल रहा था।
उदयगिरी का महास्तूप

कुछ दूरी पर ईंटों का बना एकल स्तूप खड़ा था। कुछ और आगे बढ़ने पर हम उस स्तूप तक पहुंचे। यह छोटा सा स्तूप लगभग इतनी ही ऊंची एक पीठिका पर स्थापित है। इसके आधार तक पहुँचने के लिए कुछ अर्धगोलाकार सीढ़ियाँ थी। बड़े वृक्षों के मध्य स्थित यह स्तूप अत्यंत मनोहारी दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। ऊपर चढ़कर हमने देखा कि स्तूप के चारों ओर भित्ति पर बुद्ध की प्रतिमाएं हैं जो उन्हे उनके चार जीवन मुद्राओं में दर्शाती हैं। वे मुद्राएं हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वरद मुद्रा तथा धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा।
यह एक छोटा पूर्वमुखी बौद्ध विहार है।
उदयगिरी का बौद्ध विहार?

यहाँ से हम उदयगिरी के दूसरे बौद्धस्थल पहुंचे जो एक बौद्धमठ था। यहाँ उजले रंगों से सज्ज एक छोटे से देवी मंदिर ने हमें कृतार्थ कर दिया। मंदिर के उस पार खंडहर था। द्वार की एक अलंकृत चौखट थी जो सूक्ष्मता से उत्कीर्णित थी। इसे देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह मठ का एक महत्वपूर्ण भाग था जो अब तक अखंडित बचा हुआ है। इसके भीतर भगवान बुद्ध की कुछ मूर्तियाँ थीं जो विभिन्न स्तर पर खंडित थीं। इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ था जिस पर मेहराब युक्त झरोखे थे।
इसके चारों ओर आप विभिन्न कक्षों के अवशेष में इसकी मूल आकृतियों की झलक देख सकते हैं। बौद्ध भिक्षु इन कक्षों में रहते थे। प्रथम तल पर भी कक्षों की आकृतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं जिन्हे देख ऐसा जान पड़ता है कि यह मठ विभिन्न तलों में निर्मित था।

मठ के चारों ओर स्थित जल की नहर यह बताती है कि उस समय जल संचयन, प्रयोग एवं निकासी की उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध थी। एक गोलाकार संरचना ने मुझे दुविधा में डाल दिया। मैं विचार करने लगी कि किसी समय यह कुआँ था अथवा किसी भंगित स्तूप का आधार।
मठ के ऊपर से आप अनेक बड़े-छोटे स्तूप देख सकते हैं। उनके ऊपर की सपाट सतहों को देख यह कल्पना करना कठिन है कि इनके शीर्ष सदा से सपाट थे अथवा काल के थपेड़ों को सह कर धराशायी हो गए हैं। अपनी दृष्टि को दूर तक खींचे तथा उस पार खड़ी पहाड़ी की ढलान पर देखें तो आपको ऐसी ही अनेक संरचनाएं दृष्टिगोचर होंगी। वहाँ कदाचित एक अन्य मठ तथा उससे संबंधित कुछ स्तूप हैं।

देवी मंदिर के भीतर तीन प्राचीन पाषाण की मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर के अतिरिक्त, बावड़ी के समीप भी एक छोटा सा मंदिर है। केवल ये दोनों मंदिर ही इस क्षेत्र की जीवंत संरचनाएं हैं।
शिलाओं से बनी बावड़ी
मेरे लिए इस मठ का सर्वाधिक स्मरणीय भाग यहाँ की बावड़ी थी जिसे पत्थर को काटकर बनाया गया था। इसके अनोखे आकार ने मुझे चकित कर दिया था। बावड़ी चौकोर थी किन्तु इसकी ओर जाती सीढ़ियाँ एक लंबी घटिका अथवा गर्दन के समान थी। समीप लगा सूचना पटल हमें जूते-चप्पल पहनकर जल में प्रवेश ना करने की चेतावनी तो दे रहा था परंतु उस पर इस अनोखी पाषाणी बावड़ी के विषय में जानकारी के नाम पर लेश मात्र भी उल्लेख नहीं था।

मैं यहाँ जनवरी के मध्य में आई थी किन्तु उस समय भी बावड़ी में नाममात्र जल था। बावड़ी की भीतरी भित्तियों पर कुछ आले थे। कदाचित किसी काल में उनके भीतर प्रतिमाएं रखी हों।
मठ स्थल पर कोई भी दिशानिर्देशक पुस्तिका उपलब्ध नहीं थी, न ही कोई परिदर्शक उपलब्ध था जो हमें इस स्थान के विषय में बता सकता। एक चौकीदार अवश्य था जो पूछने पर गाइड का कार्य भी कर रहा था। जल एवं भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। कदाचित शौचालय उपलब्ध हो। वाहन स्थानक से यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ दूर चलना भी पड़ता है।
इस मठ को विस्तृत रूप से अवलोकन करने के लिए एक घंटे का समय पर्याप्त है।
अवश्य पढ़ें: ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के २४ विशेष आकर्षण
रत्नागिरी
रत्नागिरी उदयगिरी के समीप ही स्थित है। अतः उदयगिरी के पश्चात हमारा अगला गंतव्य रत्नागिरी ही था। नीचे एक टिकट खिड़की है जहां से अनेक छोटी छोटी सीढ़ियों वाली लंबी पगडंडी को पार कर आप एक पहाड़ी पर पहुंचेंगे। ऐसा कहा जाता है कि रत्नागिरी पहाड़ी तीन नदियों से घिरी हुई है, ब्राह्मणी, किमिरिया एवं बिरुपा। किन्तु इस पुरातत्व स्थल के समीप मुझे किसी नदी के चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हुए। यदि समीप नदियां थीं अथवा अब भी हैं तो कदाचित यही कारण हो कि बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ मठ की स्थापना की थी।

यद्यपि इसकी सर्वप्रथम खोज सन् १९०६ में हुई थी तथापि इस स्थान का उत्खनन १९५८ में ही हो पाया था। यूँ तो रत्नागिरी का यह मठ स्थल १६वीं सदी तक अस्तित्व में था, किन्तु यह स्थल ५वीं से १२वीं सदी के मध्य सर्वाधिक सक्रिय था। यहाँ से प्राप्त धातु की कुछ कलाकृतियों को देख कर इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि यह तांत्रिक अनुष्ठानों का स्थल था। यहाँ के उत्खनित मिट्टी की एक पटलिका से यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस स्थान को ‘श्री रत्नागिरी महाविहारिए आर्य भिक्षु संघश्य’ कहा जाता था। शीर्ष पर पहुँचने के पश्चात जो दृश्य सर्वप्रथम आपको आकर्षित करती है, वह है बायीं ओर स्थित इच्छापूर्ति के छोटे छोटे अनेक स्तूपों की शिस्तबद्ध पंक्तियाँ। स्तूप तो प्राचीन हैं किन्तु इन शिस्तबद्ध पंक्तियों की व्यवस्था नवीन प्रतीत होती है। ये इच्छापूर्ति के द्योतक हैं। यहाँ से एक मिट्टी की पगडंडी दाहिनी ओर जाती हुई हमें एक छोटे मठ तक ले जाती है जो ११वीं -१२वीं सदी का है। यहाँ देखने योग्य अधिक कुछ नहीं है किन्तु इसे देखकर मठ की मूल संरचना के विषय में जानकारी अवश्य प्राप्त होती है।

इच्छापूर्ति स्तूपों के बायीं ओर स्थित एक मार्ग हमें मुख्य मठ की ओर ले जाता है। यह मठ भी इच्छापूर्ति के छोटे छोटे अनेक स्तूपों से घिरा हुआ है।
बड़ा मठ अर्थात् मठ क्रमांक १

इस क्षेत्र का सर्वोच्च आकर्षण एक बौद्ध मठ है। हरे क्लोराइट पत्थर में बने एक अप्रतिम उत्कीर्णित द्वार से आप इसके भीतर प्रवेश करते हैं। इसकी भित्तियाँ विभिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमाओं से अलंकृत हैं। उनमें एक प्रतिमा देवी यमुना की भी है। इसके भीतर जाते ही आप एक बड़े मुक्त प्रांगण में पहुंचते हैं। प्रांगण के चारों ओर स्थित भित्तियों पर बुद्ध एवं बोधिसत्व की प्रतिमाएं हैं। बुद्ध के शीश की भी अनेक प्रतिमाएं हैं जिनमें अधिकांश की नासिका भंगित है। कई भंगित भाग ऐसे हैं जो किसी समय किसी विशाल प्रतिमा का भाग रहे होंगे, जैसे विशाल चरण। अपने पैर उसके समीप रखें तो आकार की विशालता आपको अचंभित कर देगी। विभिन्न भागों को जोड़कर कुछ प्रतिमाओं को पुनः निर्मित करने का प्रयास अवश्य किया गया है किन्तु उन्हे देख आसानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये भाग भिन्न भिन्न प्रतिमाओं के हैं।

मुख्य गर्भगृह के द्वार की चौखट भी उत्कृष्ठता से उत्कीर्णित है। इसके भीतर भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है। इसकी नासिका के अतिरिक्त यह प्रतिमा लगभग अभंगित है। इसकी नासिका को देख यह आभास होता है कि किसी समय इस प्रतिमा के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। बुद्ध की प्रतिमा के दोनों ओर दो द्वारपालों की खड़ी प्रतिमाएं हैं।

एक ओर ६ छोटे मंदिरों की पंक्ति है जिसके मध्य एक सुंदर द्वार है। अब ये पावन कक्ष रिक्त हैं। स्वयं का छायाचित्र लेने के लिए यह उत्तम पृष्ठभूमि हो सकती हैं। उन्हे देख अनेक विचार मेरे मन में विचरण करने लगे थे, क्या ये छोटे मंदिर आरंभ से यहीं थे, क्या इनके भीतर कभी कोई मूर्तियाँ थीं अथवा कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर की भांति क्या ये ध्यान स्थल थे, इत्यादि।
विशाल मुक्त प्रांगण के मध्य खड़े होकर मैं कल्पना के सागर में गोते लगाने लगी। अनेक भिक्षु यहाँ बैठकर ध्यान कर रहे हैं अथवा अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे दृश्य मेरे नेत्रों में तैरने लगे थे।
मठ क्रमांक २ एवं ३

मुख्य मठ से लगा हुआ ही एक अन्य मठ है जो अब खंडित हो चुका है। आप यहाँ कुछ स्तूप देख सकते हैं। उनमें से एक स्तूप पर तीन तलों का हर्मिका अर्थात् ग्रीष्मभवन अब भी लगभग अखंडित रूप से विद्यमान है।
तीसरा मठ एक कोने में है जिसमें छोटे-बड़े अनेक स्तूप हैं।
धर्म महाकाल मंदिर

कुछ आगे जाकर, मठ से एक तल नीचे, एक सादा किन्तु प्राचीन शिव मंदिर है। पत्थर में निर्मित इसकी ठेठ वक्रीय संरचना इसकी विशेषता है। इसे देख यह एक जीवंत मंदिर प्रतीत होता है। इंटरनेट से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे मुख्य स्थल से स्थानांतरित कर यहाँ पुनः स्थापित किया है।
रत्नागिरी स्थल संग्रहालय

इस पुरातात्विक स्थल से लगा हुआ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक संग्रहालय है जहां इस पुरातात्विक स्थल से उत्खनित अनेक कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। इसकी चार दीर्घाओं में इच्छापूर्ति स्तूप हैं तथा शिला, कांस्य, तांबा, हस्तिदंत इत्यादि में बनी अनेक प्रतिमाएं हैं। शिलाखंड एवं तांबे के पत्रकों में अनेक अभिलेख हैं। टेरकोट्टा(पकी मिट्टी) की अनेक मुद्रिकाएं हैं। बुद्ध, बोधिसत्व, अपराजिता, अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, तारा, कृष्ण-यमारि इत्यादि की प्रतिमाएं हैं।
यह संग्रहालय शनिवार से ब्रहस्पतिवार तक प्रातः ९ बजे से संध्या ५ बजे तक खुला रहता है। अधिक जानकारी के लिए इस वेबस्थल से संपर्क करें।
अवश्य पढ़ें: ओडिशा के जाजपुर का बिरजा देवी शक्तिपीठ
ललितगिरी
ललितगिरी को नल्तिगिरी भी कहा जाता है। ललितगिरी अन्य दोनों स्थलों से कुछ दूरी पर स्थित है। यह स्थल तीनों स्थलों में से सबसे छोटा किन्तु सबसे उत्तम संवर्धित स्थल है। इसका उत्खनन सर्वप्रथम सन् १९७७ में किया गया था। तब से अब तक यहाँ से अनेक जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त टेरकोट्टा(पकी मिट्टी) की एक मुद्रिका के अनुसार इस स्थल का आधिकारिक नाम श्री चंद्रादित्य विहार समग्र आर्य भिक्षु संघ था।

ललितगिरी पुरातत्व स्थल के उत्खनन का चरमोत्कर्ष क्षण था यहाँ के स्तूपों के भीतर बौद्ध अवशेषों की खोज। ये अवशेष एक छोटे सुनहरे डिब्बे में रखे हुए थे। इस डिब्बे को एक के ऊपर एक अनेक डिब्बों में बंद किया हुआ था।
ललितगिरी को ओडिशा के सर्वाधिक आरंभिक काल के बौद्ध स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ से प्राप्त प्रमाणों के अनुसार यह स्थल ३री सदी से १०वीं सदी तक सक्रिय था।
महास्तूप
ललितगिरी में एक पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल स्तूप है। वहाँ तक पहुँचने के लिए लंबी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। वहाँ से पहाड़ियों से भरा आसपास का दृश्य अत्यंत मनोहारी प्रतीत होता है।

स्तूप के नाम पर वहाँ एक ऊंची पीठिका पर ईंटों की गोल संरचना है। कुछ प्रतिमाएं यहाँ-वहाँ बिखरी हुई हैं किन्तु उन्हे पहचानना कठिन है।
यहाँ का चैत्यगृह विशाल है। यद्यपि अब आप इसकी केवल रूपरेखा ही देख सकते हैं, तथापि आप कल्पना कर सकते हैं कि यह अत्यंत सुंदर स्थल रहा होगा। चैत्यगृह चार छोटे मठों से घिरा हुआ है। चारों ओर मनौती स्तूप बिखरे हुए हैं।
यहाँ की पक्की पगडंडियों पर चलते हुए आप इस ऊंचाई से दूर पर ललितगिरी का सम्पूर्ण मठ देख सकते हैं। किन्तु भीतर जाकर सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य खो सा जाता है।
ललितगिरी में एक आधुनिक स्थल संग्रहालय है। किन्तु यहाँ छायाचित्रीकरण की मनाही है। किसी प्रकार की विवरणिका पुस्तिका भी उपलब्ध नहीं है।
पुष्पगिरी विश्वविद्यालय
ऐसा माना जाता है कि पूर्व में ये तीनों स्थल एक साथ पुष्पगिरी विश्वविद्यालय का भाग थे जो अब किसी अन्य स्थान में लांगुड़ी नाम से स्थित है। पुष्पगिरी का उल्लेख ह्वेन त्सांग के यात्रा विवरणों में भी प्राप्त होता है।
पर्यटन की दृष्टि से उदयगिरी, रत्नागिरी एवं ललितगिरी ओडिशा के त्रिकोणीय माणिक्य के नाम से लोकप्रिय हैं।
अवश्य पढ़ें: हीरापुर ओडिशा का चौसठ योगिनी मंदिर ९ वीं. सदी का अद्भुत माणिक्य
यात्रा सुझाव
- अधिकार पर्यटक भुवनेश्वर में ठहरकर इन स्थलों का एक-दिवसीय भ्रमण करते हैं। हमने भुवनेश्वर से भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जाते समय, मार्ग में इन स्थलों का भ्रमण किया था।
- केवल रत्नागिरी में ही ओडिशा पर्यटन विभाग का अतिथिगृह है जहां भोजनालय भी है। अन्य स्थानों की सुविधाएं सीमित हैं।
- प्रवेश शुल्क नाममात्र है।
- इन सभी पर्यटन स्थलों में छायाचित्रीकरण की पाबंदी नहीं है।
















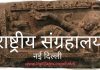

Hi ..this is nice informatavive blogs about odisha. I am searching for this type of information. Thanks for sharing.