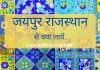मानवी चेतना के आरंभ से मनुष्य प्रकृति के विभिन्न रूपों की आराधना करता आ रहा है। मनुष्य ने अपनी कल्पना में प्रकृति के अनेक दैवी रूपों को प्रकट किया है। देव सदृश प्रकृति की ओर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने में वह सदैव आनंद का अनुभव करता आया है। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, उसकी प्रथाओं में परिवर्तन होते गए। अब मनुष्य प्रकृति से प्राप्त विभिन्न पदार्थों का अर्पण कर भगवान के दिव्य रूप की आराधना करने लगा है। यह प्रथा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अब भी वनस्पति एवं जीव-जंतुओं से संबंध रखती है। फूल बंगला ऐसी ही एक प्रथा है जिसमें प्रकृति का उत्सव मनाया जाता है।
भारत में प्रकृति से प्राप्त लगभग सभी पदार्थों को भगवान को अर्पित करने के लिए सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। उनमें पुष्पों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विशेष चढ़ावा जाना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं:
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति।
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः।।9.26।।
हे अर्जुन! जो भी भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि भक्ति से अर्पण करता है, उस शुद्ध मन के भक्त द्वारा वह भक्तिपूर्वक अर्पण की गई भेंट मैं प्रेम से स्वीकार करता हूँ।
वेदों, उपनिषदों, पुराणों जैसे सभी प्राचीन ग्रंथों ने प्रकृति एवं उसके विभिन्न रूपों की आराधना की परम महत्ता को विस्तृत रूप से उजागर किया है। इस परिप्रेक्ष्य में ब्रज का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। सम्पूर्ण कृष्ण लीला किसी ना किसी रूप में प्रकृति के चारों ओर ही केंद्रित थी। गोवर्धन, यमुना, वृंदा, गऊ इत्यादि प्रकृति के वे प्रतिनिधि हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण के जीवन में विशेष भूमिकाएं निभायी हैं।
फूल बंगला प्रथा का इतिहास

१६ वीं. सदी में भारत में भक्ति आंदोलन का समय था जब सम्पूर्ण भारत से अनेक साधू-महात्मा ब्रजभूमि आए थे। उस समय विद्यमान राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थिति में कृष्ण भाव पुनः स्थापित करने में ब्रज का अविस्मरणीय योगदान रहा है। इन साधु-महात्माओं ने ब्रज में विद्यमान वृक्ष वाटिकाओं एवं उपवनों में प्रकृति की प्रचुरता को मुक्त हृदय से स्वीकार किया था। उन्होंने चारों ओर स्थित प्रकृति को अपने दैनिक अनुष्ठानों एवं सेवाओं का अभिन्न अंग बना लिया था।
धर्म गुरुओं द्वारा आरंभ किये गए अनेक पंथों ने किसी ना किसी रूप में प्रकृति को अपनी रीति से भगवान की आराधना का अभिन्न अंग बनाया है। इस प्रथा के चलते ब्रज की पावन भूमि में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके साथ ही ब्रज में अनेक पारंपरिक एवं सांस्कृतिक कला शैलियाँ विकसित एवं पोषित हुईं जिनके द्वारा भगवान को सेवा अर्पित की जाती थी। इस प्रकार की गई भगवान की सेवा ने अनेक सांस्कृतिक शिल्पों एवं कला शैलियों को विकसित होने का अवसर प्रदान किया। रथयात्रा में प्रयुक्त भव्य रथ, झूला यात्रा में प्रयोग किया गया झूला इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं। इस संस्करण में हम भगवान की जिस सेवा का उल्लेख कर रहे हैं वह है वृंदावन व ब्रज के मंदिरों में पुष्प सज्जा, जिसे फूल बंगला भी कहा जाता है।
धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च॥
– पद्म पुराण, भागवत माहात्म्य (1.61)
धन्य है वृंदावन की पावन भूमि, जहाँ भक्ति सम्पूर्ण परमानन्द में नृत्य करती हैं।
वृंदावन का भक्ति नृत्य सर्वोच्च परमानन्द का प्रतीक है। यह विविध पूजा अनुष्ठानों का परिणाम है जिन्हे उस काल के विभिन्न आध्यात्मिक महानुभावों ने आरंभ किया था। इसी की स्पष्ट झलक हमें ब्रज भूमि के अनेक सांस्कृतिक कलाओं में आज भी दृष्टिगोचर होती हैं।
वृंदावन का फूल बंगला
वृंदावन की वर्तमान फूल बंगला परंपरा प्राचीन अनुष्ठानिक परंपरा की ही निरन्तरता है। यद्यपि यह फूल बंगला सम्पूर्ण ब्रज में बनाया जाता है एवं इसका उत्सव मनाया जाता है, तथापि परंपरा में विविधता के कारण वृंदावन में इसे विशेष सम्मान प्रदान किया जाता है।
१६ वीं. सदी के साहित्यों में फूल महल, फूल कुंज, फूल भवन तथा फूल बैठक जैसे शब्दों का उल्लेख है। फूल बंगला, यह शब्द १७ वीं. सदी के साहित्यों में देखा गया है। हरिभक्तिविलास, केलीमाल, हित चौरासी तथा सुरसागर जैसे मध्यकालीन ग्रंथ भी फूल बंगला अनुष्ठान की, भगवान को अर्पित सेवा के रूप में, विस्तृत चर्चा करते हैं।
हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पुष्प सज्जा उन ६४ कलाओं में से एक है जिसे मनुष्य आत्मसात कर सकता है। मानवी भावनाओं एवं धार्मिक संस्कारों का यह अद्भुत संगम ब्रज को एक अप्रतिम आभा प्रदान करता है। ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती उष्णता में ब्रज के दैवी वनों के प्राकृतिक परिदृश्यों को पुनर्सृजन करने का यह प्रयास, वास्तव में मंदिर की प्रतिमाओं को सुवासित पुष्पों की शीतलता द्वारा सुख प्रदान करने की एक चेष्टा है। मंदिरों में किये जाने वाली इस पुष्प सज्जा का मूल सिद्धांत भी यही है।
फूल बंगला कब मनाया जाता है?
यह उत्सव चैत्र शुक्ल एकादशी अर्थात् अक्षय तृतीया से आरंभ होकर हरियाली तीज से एक दिवस पूर्व समाप्त होता है। अर्थात् यह उत्सव वैशाख, ज्येष्ठ तथा आषाढ़, ये तीन मास की अवधि तक मनाया जाता है। अंग्रेजी पंचांग के अनुसार यह अवधि अप्रैल के मध्य से जुलाई के मध्य तक होती है।
इस पुष्पोत्सव के दर्शन करने का एवं इसका आनंद उठाने का सर्वोत्तम समय ग्रीष्मऋतु है क्योंकि इस समय प्रचुर मात्रा में पुष्प उपलब्ध होते हैं। जैसे ही वर्षा ऋतु आरंभ होती है, पुष्प सजावट का आकार छोटा होने लगता है। वर्षा ऋतु में पुष्पों की आवक घट जाती है जिससे फूल बंगले की सज्जा में प्रयुक्त पुष्पों की प्रचुर मात्रा की आपूर्ति नहीं हो पाती।

इस पुष्प सज्जा में विशेषतः बेला अथवा चमेली पुष्प का सर्वाधिक प्रयोग होता है। गुलाब एवं गेंदे के पुष्प तथा अशोक वृक्ष की पत्तियों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। केले के तने की छाल को उत्कीर्णित कर भी इस सज्जा में प्रयोग किया जाता है। वृंदावन के विभिन्न धार्मिक समुदायों के अभिलेखों व ग्रंथों में विविध प्रकार के पुष्पों का उल्लेख किया गया है जो १६ वीं. सदी से अब तक इस पुष्प सजा की कला को प्रभावित करते आए हैं। वृंदावन के लगभग सभी मंदिर इस परंपरा का पालन करते हैं। उनमें से कुछ लोकप्रिय मंदिर हैं, बाँके बिहारी जी, राधावल्लभ जी, राधारमण जी, राधादामोदर जी, रंग जी, राधाश्याम सुंदर जी, भट्ट जी इत्यादि।
फूल बंगला कैसा दिखता है?
लकड़ी के भिन्न भिन्न आकार के चौखटों को व्यवस्थित रीति से लगा कर एक अस्थायी संरचना निर्मित की जाती है। इसे स्थानीय भाषा में थाट कहते हैं। तत्पश्चात विभिन्न पुष्पों द्वारा अलंकृत कर इस अस्थायी संरचना को एक मंदिर का रूप दिया जाता है। संध्या के समय भगवान के विग्रह अथवा मूर्ति को पुष्प के मंदिर के भीतर बिठाया जाता है। रात्रि तक मूर्ति इस पुष्प मंदिर में ही विराजमान रहती है।

फूल बंगले की चौखटों को विभिन्न नामों से पहचाना जाता है, जैसे छज्जा, पिछवाई, हाथी, बगली इत्यादि। इनके नामों से आप भी इन्हे पहचान गए होंगे। रूपरेखा के अनुसार इन चौखटों को अपने अपने स्थानों पर बिठाया जाता है। इन चौखटों की किनारियों पर आवश्यकतानुसार कीलें गढ़ी होती हैं। कलाकार इन कीलों की सहायता से एवं रूपरेखा के अनुसार चौखटों पर बेला पुष्प की लंबी लंबी लड़ियाँ सजाते हैं। चौखटों की व्यवस्था जगमोहन की आकृति एवं माप के अनुसार की जाती है जो गर्भगृह के ठीक बाहर का क्षेत्र होता है।


केले के तने की छाल द्वारा अलंकरण

केले के तने की छाल से अलंकरण करने के लिए तने के सबसे भीतरी भाग को सावधानी पूर्वक निकाला जाता है। इन्हे विभिन्न आकृतियों में काटकर चौखटों पर लगाया जाता है। एक बड़ा फूल बंगला बनाने के लिए ६ से १० लोगों को लगभग ४ से ६ घंटों का समय लग जाता है। वर्तमान में वृंदावन तथा वृंदावन के बाहर स्थित ब्रज के अन्य मंदिरों में कलाकारों के ६ से ७ ऐसे समूह हैं जिन्होंने यह पारंपरिक पुष्प सज्जा बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
१८ वीं. शताब्दी में श्री प्रेमदास जी द्वारा ब्रज भाषा में रचित यह प्रसिद्ध दोहा इस परंपरा की सुंदरता का बखान करता है:
मोतिया की जाली में गुलाब ही के फूल खांचे, बंगला में रचे सोनजूही के से द्वार है
कंज के कमल राजे माधवी के छज्जा छान्जे, पीत चमेली के लटकन अति चारु है
फूल के सिंघासन पे फूल रहे श्यामा श्याम, फूलन के अभिराम शोभित शृंगार है
प्रेमदास हित वारी फूली अति फुलवारी, कुंज केली फूली भारी फूले रतिमार है
उत्सव क्षेत्र

वृंदावन उत्सवों की धरती है। वृंदावन में कदाचित एक भी ऐसा दिवस नहीं होगा जब किसी उत्सव अथवा अनुष्ठान का आयोजन नहीं किया जा रहा हो। ब्रज की भक्ति परंपरा में कहावत है, भाव ग्राही जनार्दन। इसका अर्थ है कि भाव से अर्पित सभी पदार्थ भगवान कृष्ण सहर्ष स्वीकार करते हैं। वृंदावन भक्ति का प्रतीक है। इस प्रथा का आनुष्ठानिक दृष्टिकोण मुख्यतः उष्ण वातावरण में भगवान को सुख एवं समाधान प्रदान करने की भावना है जो एक भक्त के हृदय को तृप्त करता है।
अन्याभिलाषिता-शून्यम ज्ञान-कर्मध्यानवृतम,
अनुकुल्येन् कृष्णानुसील नम् भक्ति-उत्तम।
— श्री भक्ति-रसामृत-सिंधु (१.१.११)
संक्षेप में इसका अर्थ है, जब कृष्ण की सुख-सुविधा के लिए कोई सेवा अर्पित की जाती है तो वह सेवा भक्ति की चरम सीमा मानी जाती है।
वृंदावन सदा से सेवभाव की भूमि रही है। वृंदावन के कोने कोने में वर्षों से यह सेवा भाव देखा जा रहा है। सेवा वृंदावन के आनुष्ठानिक स्वरूप का अखंड भाग है। वृंदावन के मंदिरों को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों से जोड़ने में यही सेवा भाव उत्प्रेरक है। यह भगवान एवं एक भक्त के मध्य के सुमधुर संबंध का परम प्रतीक है।
इस संस्करण में प्रयुक्त अधिकांश छायाचित्र निशांत शर्मा फोटोग्राफी के सौजन्य से प्राप्त किये गए हैं। उन अप्रतिम छायाचित्रों के लिए उनका विशेष आभार!!!
राधे-राधे !!!
यह सुशांत भारती द्वारा अभिदत्त एक अतिथि संस्करण है।
सुशांत भारती एक संरक्षण वास्तुकार हैं। उन्होंने वास्तुकला अकादमी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से वास्तुशास्त्र में स्नातक के उपाधि तथा नई दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लैनिंग एण्ड आर्किटेक्चर से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। भारत के विभिन्न सांस्कृतिक आयामों के शोध में उनकी विशेष रुचि है। वास्तु विविधता के साथ साथ उनके शोध के मूल विषय हैं, ‘ब्रज की सांस्कृतिक धरोहर’ एवं ‘भारतीय मंदिर वास्तुकला’। वर्तमान में वे नई दिल्ली के जनपथ पर स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान में रिसर्च असिस्टन्ट के पद पर कार्यरत हैं।
सुशांत भारती द्वारा लिखा यह संस्करण अवश्य पढ़ें – RasikPriya – The Geet Govind of Bundelkhand