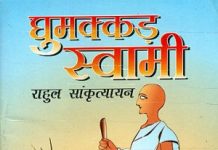श्री राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित पुस्तक “वोल्गा से गंगा” एक महाकाव्य है। यह ६००० ई.पू. से लेकर १९४२ ई. तक की समयावधि में हुए मानव विकास का, सामान्य जनमानस की दृष्टी से अनुरेखण करता है। इस पुस्तक में लेखक ने मानव जाति के विकास का चित्रण, वोल्गा नदी के तीर से, उस काल से किया है जब मानव एक शिकारी था। लेखक ने विभिन्न युगों में हुए मानव विकास को उस युग से सम्बंधित लघु कथाओं के माध्यम से अत्यंत क्रमवार पद्धति से वर्णित किया है। यद्यपि पुस्तक का उत्तरार्ध अधिकांशतः भारतीय उपमहाद्वीप पर केन्द्रित है, उन्होंने सम्पूर्ण विश्व की विषयवस्तु को ओझल नहीं होने दिया। सम्पूर्ण पुस्तक पढ़ने के पश्चात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आदिकाल से भारत के साथ साथ सम्पूर्ण विश्व उतना ही सार्वभौमिक था जितना वर्तमान में है।
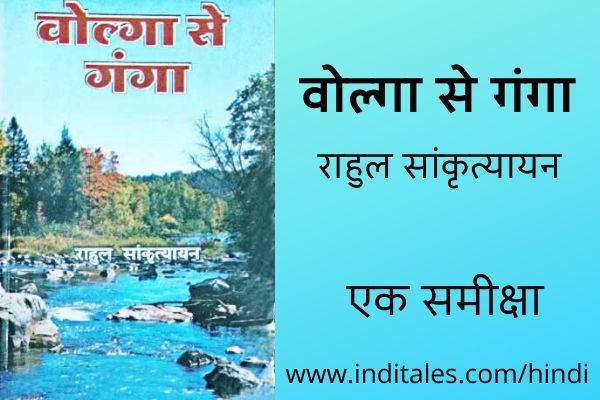
लेखक राहुल सांकृत्यायन ने विषय वस्तु को प्रत्येक स्तर पर छुआ है। सामान्य जनमानस के संवादों के सहारे वे प्रत्येक काल के जनजीवन का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे हैं। पुस्तक के अनुसार समयावधि के आरंभिक काल में स्त्रीप्रधान समाज हुआ करता था जिसका जीवन मांस तथा जल पर निर्भर था। उस मातृप्रधान समाज में वंश का उत्तरदायित्व माता से पुत्री को प्राप्त होता था। मध्यकालीन युग में राजाओं का जैसा सम्बन्ध उनके पुत्रों से था, ठीक वैसा ही सम्बन्ध इस समाज में माताओं का उनके पुत्रियों से होता था। इस काल में उत्तराधिकार हेतु पुत्रियों के बीच मनमुटाव तथा झगड़े भी होते थे। शनैः शनैः खेतीबाड़ी ने मानव के जीवन में पदार्पण किया।
राहुल सांकृत्यायन रचित वोल्गा से गंगा यहाँ अमेज़न पर लें
इस पुस्तक के जिस विषय ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया, वह था धातु का आगमन। प्रथम लौह, तत्पश्चात स्वर्ण। उसके साथ आयी भेदभाव नीति। राहुल सांकृत्यायन ने अत्यंत विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है कि किस प्रकार से धातु समाज को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटने लगी थी। समाज का वर्गीकरण आरम्भ होने लगा था कि किस वर्ग का अधिकार किस धातु पर व कितनी मात्रा पर होगा। मध्यकालीन युग की कथाओं के पात्रों को जिस प्रकार से स्वामित्व हेतु वादविवाद करते दर्शाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है मानो यह वर्तमान के समाज का दृश्य हो। फिर वह किसी भी नवीन आविष्कार के पश्चात उस पर आर्थिक आधार पर अधिपत्य की होड़ हो अथवा उस आविष्कार का समाज पर नकारात्मक प्रभाव की चर्चा हो।
इसका ज्वलंत उदाहरण हम सबने कई बार देखा अपने ही जीवन काल में, जैसे दूरदर्शन, कंप्यूटर अथवा संगणक, मोबाइल फ़ोन इत्यादि। शनैः शनैः ये सर्व आविष्कार हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनने लगते हैं। कुछ समय पश्चात हमें यह स्मरण भी नहीं रहता कि कभी इन अविष्कारों ने भरपूर हलचल मचायी थी। यह पुस्तक आदि काल से उपस्थित समाज के इस आयाम को अत्यंत सूक्ष्मता से चित्रित करती है। कदाचित समाज का प्रत्येक महत्वपूर्ण युग इन अवरोधों का संग्रह ही है।
राहुल संकृत्यायन का घुम्मकड़ शास्त्र
वोल्गा से गंगा, इस पुस्तक के आरंभिक कुछ अध्याय पूर्व-ऐतिहासिक इतिहास का वर्णन करते हैं। इन अध्यायों की रचना हेतु लेखक राहुल सांकृत्यायन को अपनी कल्पना शक्ति का भरपूर उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी होगी। बाद के अध्याय मुझे उपलब्ध साहित्यों पर आधारित प्रतीत हुए। पुस्तक का अंतिम अध्याय कदाचित लेखक के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा रचित है।
पुस्तक में विषयवस्तु का समाजवाद की ओर झुकाव स्पष्ट झलकता है। समाजवाद प्रत्येक युग की विशिष्टता थी। समाज में प्रायः गाँधी तथा आंबेडकर को आधुनिक समाज के रचयिता माना जाता है। परन्तु इस पुस्तक में गाँधी तथा अम्बेडर के विषय में लोगों के विपरीत दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किये गये हैं। आप जनता के इस विपरीत दृष्टिकोण पर संशय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यह पुस्तक स्वंत्रता पूर्व लिखी गयी थी। यहाँ तक कि पटना का एक सामान्य मनुष्य स्वयं को हरिजन गाँधी कहने में लज्जा अनुभव करता था। उस काल में कई लोग आंबेडकर के सिद्धांतों से भी सहमत नहीं थे। उनकी भावनाएं इतनी तीव्र थीं कि यह वर्तमान के पंडितों हेतु भी आश्चर्य का विषय हो सकता है।
यूँ तो मुझे वोल्गा से गंगा, यह पुस्तक सम्पूर्ण रूप से रुचिकर प्रतीत हुई, यद्यपि इसका एक अध्याय मुझे विशेषतः प्रिय लगा। यह अध्याय राजा हर्षवर्धन द्वारा शासित उज्जैन नगर पर आधारित है। इस अध्याय में उस काल का वर्णन राजा, राज-कवि तथा एक सामान्य मनुष्य तीनों के दृष्टिकोणों से किया गया है। इसमें राज-कवि के उत्तरदायित्व का चित्रण किया गया है। राज-कवि राजा की छवि एक आदर्श शासक के रूप में गढते थे, आकर्षक व्यक्तित्व, वीर, दयालु तथा न्यायप्रिय इत्यादि। राजा की छवि तथा उनके महल का चित्रण वास्तविक ना होते हुए काल्पनिक स्तुति गायन अधिक होते थे। इस अध्याय को पढ़कर आप सोच में पड़ जाते हैं कि कवि की प्रशंसा की जाए, या राजा व उनके राजपाट की सराहना अथवा किसी पर भी विश्वास ना किया जाय।
लेखक ने इस पुस्तक में समय के साथ आये मानवी संबंधों का भी पर्याप्त उल्लेख किया है। आरम्भ में बंजारों अर्थात् खानाबदोश जाति के विषय में उल्लेख है। मानवी संबंधों के नाम पर ये घुमंतू बंजारे केवल स्त्री पुरुष के मध्य यौन सम्बन्ध तथा एक माता के अपनी संतान के साथ ममता तक ही सीमित थे। जब मानव घुमक्कड़ी त्याग कर खेतीबाड़ी से जीवन यापन करने लगा तब उनके आपसी सम्बन्ध भी पशु प्रकृति छोड़कर पारिवारिक संबंधों में विकसित होने लगे। प्रेम जैसे कोमल भावनाओं ने जन्म लेना प्रारम्भ किया। इन्ही परिवर्तनों को लेखक ने अपनी कथाओं के सहारे मनमोहकता से प्रतिपादित किया है। प्रेम उनकी कहानियों का अभिन्न अंग हैं। रिश्तों में छलकपट तथा धोखे को उन्होंने अपनी कहानियों में सम्मिलित नहीं किया है। मानवी संबंधों में एक पड़ाव आगे जाते हुए उन्होंने विभिन्न समुदायों तथा विरोधियों के मध्य संबंधों की भी सुन्दर व्याख्या की है। इसी प्रकार परिवारों तथा मित्रों के मध्य संबंधों को भी खोजने का प्रयत्न किया है।
इस पुस्तक की एक विशेषता है कि इसमें उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का कदापि उल्लेख नहीं है जिनके विषय में हम इतिहास की पुस्तकों में पहले ही पढ़ चुके हैं। अतः आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि इस पुस्तक में बुद्ध तथा बौध धर्म के उदय का किंचित भी वर्णन नहीं है। उसी प्रकार से मानवी सभ्यताओं पर शत्रुओं द्वारा किये गए आक्रमणों पर भी उन्होंने किसी भी प्रकार से चर्चा नहीं की है। केवल इन आक्रमणों का जनसामान्य पर हुए प्रभावों पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। यहाँ तक कि गाँधी तथा आंबेडकर के व्यक्तित्व तथा उनकी उपलब्धियों का भी उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया है। कथाओं के पात्रों के मध्य साधे गए संवादों में ही कहीं कहीं इन व्यक्तित्वों के नाम उभर कर आते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कथायें महत्वपूर्ण चरित्रों तथा घटनाओं के बोझ तले दबी नहीं। आप भिन्न भिन्न कालों में स्वयं को अनुभव करते हुए उनका सजीव चित्रण स्पर्श कर सकते हैं।
यद्यपि इस पुस्तक के कई भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध हैं, मुझे इसके हिंदी अनुवाद को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी विषय में मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि इस पुस्तक के हिंदी संस्करण को समझने के लिए हिंदी भाषा में मजबूत पकड़ की अपेक्षा है। कथाओं में आपका सामना स्थानीय हिंदी भाषा के कुछ शब्दों से भी होगा जिनको समझने हेतु किंचित कल्पना शक्ति की आवश्यकता होगी। लेखन में कहीं कहीं अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।
यदि आप मेरे सामान यात्रा संस्मरण लेखन में रूचि रखते हैं तो मेरे मतानुसार इस पुस्तक में हमारी लेखनी को और अधिक धनी बनाने की क्षमता है। इतिहास के उबाऊ अध्याय को एक मनोरंजक कथा में परिवर्तित कर पाठक के मानसपटल पर अमिट छाप छोड़ना, इसका अप्रतिम उदाहरण है यह पुस्तक। इस पुस्तक में ज्ञानवर्धन हेतु भरपूर तत्व उपलब्ध है जिसे पाठक अत्यंत सहजता से ग्रहण करता है। भाषा अत्यंत लुभावनी है तथा कथानक पर लेखक की पकड़ भी पूर्णतः नियंत्रित है।
इस पुस्तक को पढ़कर मुझे अनायास ही खुशवंत सिंह की लिखी पुस्तक दिल्ली का स्मरण हो आया। उन्होंने भी उनके पुस्तक में उपरोक्त प्रारूप का उपयोग कर एक सामान्य मानव की दृष्टी से दिल्ली की कहानी कही है।
वोल्गा से गंगा, यह पुस्तक मुझे इतनी पसंद आयी कि मैं लेखक राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी अन्य पुस्तकें भी पढ़ने हेतु आतुर हो रही हूँ। इस समय मेरे निजी पुस्तकालय में उनकी दो पुस्तकें उपलब्ध हैं। प्रथम उन्हें ही पढ़ने जाती हूँ।
आप भी वोल्गा से गंगा, यह पुस्तक अवश्य पढ़े। मेरा विशवास है यह आपको भी अत्यंत मनोरंजक तथा ज्ञानवर्धक प्रतीत होगी। साथ ही आप लेखक राहुल सांकृत्यायन की अन्य पुस्तकों को पढ़ने हेतु प्रेरित होंगे।
राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यह पुस्तक, वोल्गा से गंगा आप अमेज़ोन से खरीद सकते हैं।